एक ओर हम लोग, यानी प्रगतिवादी थे, जो 'प्रगति' नाम की संस्था चलाते थे और दूसरी ओर वह लेखक वर्ग था जो वैचारिक स्वातंत्र्य की चेतना धारा के साथ अलग-अलग सा था, पर समय की धारा में सब साथ-साथ बह रहे थे। 'प्रगति' और 'एम०ए० एम०लिट० संघर्ष समिति' के बुलेटिन हम लोग स्टेंसिल काट कर साइक्लोस्टाइल कराते थे, कविता - पोस्टर बनाते थे, कंधों पर टंगा झोला प्रकाशित सामग्री से भरा रहता था। उन्हीं दिनों हिंदी विभाग के छात्रों - अध्यापकों ने 'मुट्ठियों में बंद आकार' का प्रकाशन किया जिसमें उस समय के लगभग सभी युवा रचनाकार थे। सुखबीर सिंह के संपादन में 'दिविक' निकला तो एक तरह की अखाड़ेबाजी आरंभ हो गई। अखाड़ेबाजी के इस दौर में प्रेम 'दूसरा दिविक'' में दिखाई दिए तो सुरेश ऋतुपर्ण द्वारा संपादित 'समीकरण' में भी दिखाई दिए। हमारे प्रगतिशील खेमे से अलग कृष्णदत्त पालीवाल, प्रताप सहगल, दिविक रमेश, सुरेश धींगड़ा, सुरेश किसलय, हरीश नवल, सुरेश ऋतुपर्ण, पवन माथुर, और और भी बहुत सारे साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय युवा रचनाकार थे। एक तरह की मीठी प्रतिद्वंद्विता 'प्रगति' और 'साहित्य-संगम' में रहती थी। कार्यक्रमों के लिए होता था कला संकाय का कक्ष संख्या बाइस हमें थोड़ी जद्दोजहद के साथ मिलता था, उन्हें आसानी से एक-दूसरे की गोष्ठियों में अतिथियों से प्रश्न करना और अपना ज्ञान दिखाना, ये तीरंदाजी चला करती थी। हमारी गोष्ठियों में नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर, सर्वेश्वर, प्रयाग शुक्ल, भैरों प्रसाद गुप्त, मार्कण्डेय, सव्यसाची, खगेंद्र ठाकुर, कांति मोहन, कर्ण सिंह चौहान, सुधीश पचौरी, रमेश गौड़ और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए वरिष्ठ रचनाकार आते रहते थे। इनके अलावा नए-नए साहित्यकार जैसे राज कुमार सैनी, चंचल चौहान, रमेश रंजक, महेश उपाध्याय, जोगेंद्र शर्मा, रामकुमार कृषक पुरुषोत्तम प्रतीक, बंसी लाल, कृष्ण कुरड़िया, रेखा अवस्थी आदि का जमावड़ा रहता था।
एक बार प्रेम जनमेजय ने मुझसे कहा था, "भई प्रगति के पोस्टर बहुत ही रचनात्मक और कलात्मक होते हैं।" प्रगति को एक विशेष अंदाज़ से लिखने का तरीका मैंने ही ईजाद किया था और उसका लोगो भी बनाया था। उस लोगो में एक चिंतनशील युवक ठोढ़ी पर हाथ रखे हुए है और उसके सहारे एक इंक वाला पैन है, जिसकी निब ऊर्ध्वमुखी है और समानांतर रेखाओं से चौखटे में एक संतुलन बनाया गया है। यह लोगो मेरे हाथ पर इतना सधा गया था कि मैं आँख मूंद कर भी बना सकता था। इसी तरह प्रगति भी लिखने में समस्या नहीं आती थी। मेहनत हम लोग खूब करते थे और बड़बोलेपन के शिकार रहते थे। प्रेम से जब भी चर्चाएँ हुईं, वे साहित्यकारों के बीच साहित्यिक असहिष्णुता के प्रति चिंतित दिखाई दिए। एक दूसरे से वैचारिक मतभेद हो परंतु वो खिलाड़ी भावना की तरह होना चाहिए। हम लोग उन दिनों मध्यमार्गी सोच से दूरी बना कर रखते थे। साहित्य प्राथमिक नहीं, जीवन संघर्ष प्राथमिक है, ऐसा मानते थे। कविता कहानी से ज्यादा नाटकों और नुक्कड़ नाटकों पर ध्यान देते थे। कविताएँ आंदोलनधर्मी हुआ करती थीं।
दरअसल, उस समय वैचारिक रेखाएँ इतनी तीखी और अलगाव करने वाली होती थीं कि जैसे एक परिवार में बाँट लिया जाए कि चाचा तेरा ताऊ मेरा, बुआ तेरी मौसी मेरी। इसी तरह से साहित्यकारों का बँटवारा भी कर लेते थे, उनके मन मिजाज और विचारधाराओं के रंगों के आधार पर। अपनी समन्वयवादी सोच को प्रेम ने आज तक जिंदा रखा है। उनके मित्रों के दायरे में लगभग सभी सोच के सहचर हैं। उनकी यही सोच उनके द्वारा संपादित 'व्यंग्य यात्रा' में भी दिखाई देती है। प्रेम ने 'धर्मयुग' 'सारिका' 'दिनमान' में लिखा तो प्रलेस के 'जनयुग' में भी लिखा। वे परसाई के न केवल प्रशंसक हैं, बल्कि उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं।
इकहत्तर से पिचहत्तर तक दिल्ली विश्वविद्यालय में एक जीवंत साहित्यिक वातावरण रहा। हमारी तरफ करण- सुधीश की विद्वत्ता का जलवा हुआ करता था। प्रेम जनमेजय, पवन माथुर, मुकेश गर्ग, बंसी लाल, मनीष मनोजा हम सब लोग लायब्रेरी से फैकल्टी आते हुए या फैकल्टी से लायब्रेरी जाते हुए या कभी रिसर्च फ़्लोर पर कभी सीढ़ियों पर बिन टकराए टकराया करते थे। टकराते थे हमारे विचार। लेकिन मुस्कानों के आदान-प्रदान में कभी कोई कमी नहीं आई। तल्खी नहीं आई। अपने-अपने तख्त पर बैठकर अपने-अपने विचारों की माला फेरते रहे। मालामाल होना कोई नहीं चाहता था। एक धुन थी, एक लगन थी, एक लौ थी जिसमें अपने-अपने मायने और अपने-अपने आईने लेकर बैठा करते थे। अपने आईने में उनकी सूरत दिखाते थे तो वे पलट कर अपना आइना हमारी ओर कर देते थे। इस सबमें व्यंग्य और हास्य कहाँ से फूटा ये कह पाना मेरे अपने लिए तो मुमकिन है लेकिन प्रेम के बारे में सही-सही अंदाज़ा नहीं है। हाँ, उन दिनों प्रेम के हास्य-व्यंग्य उन दिनों की प्रसिद्ध फिल्मी पत्रिका 'माधुरी' में प्रकाशित होने आरंभ हो गए थे। जिसके संपादक अरविंद कुमार थे। उन दिनों नरेंद्र कोहली धर्मयुग के बैठे-ठाले स्तंभ में विशेष चर्चित हो रहे थे। नरेंद्र कोहली प्रेम के गुरु और मार्गदर्शक हैं। प्रेम ने उनके निर्देशन में ही अपना एम०लिट० का लघु शोध प्रबंध लिखा, 'प्रसाद के नाटकों में हास्य व्यंग्य' पीएचडी भी उन्हीं के निर्देशन में की, जिसका विषय भी व्यंग्य पर ही केंद्रित था।
जैसा मैंने उपरोक्त कहा- अशोक चक्रधर के लिए मानवीय संबंध मूल्यवान हैं इसलिए वे उन्हें बोन चाईना की कॉकरी की तरह संभालकर रखते हैं, इसका उदाहरण मुझे अपने संबंधों के शैशवकाल में मिल गया था। अशोक चक्रधर एम०लिट० प्रथम वर्ष के छात्र बने थे और मैंने दूसरे वर्ष में प्रवेश लिया था। अशोक चक्रधर सुधीश पचौरी, कर्णसिंह आदि से संबंध गहरे कर रहे थे। एम०लिट० प्रथम वर्ष का परिणाम आया तो केवल मेरी प्रथम श्रेणी थी और पूरी कक्षा में किसी की नहीं थी। उस कथा में सुधीश पचौरी के अत्यधिक प्रिय मुकेश गर्ग भी थे। मुकेश गर्ग से बाद में अशोक चक्रधर के संबंध अधिक गहरे हुए सुधीश पचौरी के नेतृत्व में डॉ० नगेंद्र का किला ध्वस्त हो चुका था। सुधीश पचौरी ने हर उस चीज को, जो उनकी दृष्टि में गलत होती उसे दुरुस्त करने का बीड़ा उठा लिया था। एम०लिट० में मेरी ही प्रथम श्रेणी आई थी। सुधीश पचौरी को लगा कि विभाग ने 'केवल' प्रेम जनमेजय को प्रथम श्रेणी देकर पक्षपात किया है और अन्य विद्यार्थियों के साथ अन्याय। अब सुधीश पचौरी को अन्याय हुआ लगा तो उसका बिगुल बजना ही था। उनके सभी 'साथियों ने मुझे घेरा घारा और कला संकाय कॉफी हाउस में ले गए। वहाँ मुझ पर साम दाम दंड भेद टाइप चौतरफा आक्रमण किए गए, जिनका लक्ष्य यह था कि मैं उन्हें लिखकर दे दूँ कि मेरे प्रथम श्रेणी किसी षड्यंत्र का परिणाम हैं। चौतरफा आक्रमण चल रहे थे और मैं मौन नामक हथियार से उसका मुकाबला कर रहा था। जिस आक्रमण शैली ने डॉ० नगेंद्र का सिंहासन छीन लिया था, मेरा मुकाबला उससे था। मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ है। उसी इच्छा शक्ति से मन दृढ़ निश्चय लिया कि चाहे कुछ हो लिखकर नहीं दूँगा । इतना विश्वास था कि चाहे कितना भी डरा-धमका लें, मुझ पर शारीरिक आक्रमण नहीं करेंगे। लिखकर कुछ नहीं दिया। बाद में तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉ० विजयेंद्र स्नातक को सारी घटना सूचित की, तो चिंता की पहली रेखा दिखी और उन्होंने दो शब्द कहे- "अच्छा किया"। इस घटना को साझा करने का मंतव्य केवल इतना है कि अशोक चक्रधर के उन दिनों सुधीश पचौरी से घनिष्ठ संबंध थे पर मुझसे जुड़े संबंधों की रक्षार्थ ही संभवतः वे इस 'दुर्घटना' से दूर रहे हों। यदि वे सायास दूर रहे तो यह एक बड़ा निर्णय था। मेरा विरोध किसी वैचारिक कारण से नहीं था पर जो विरोध कर रहा था वह उस समय के दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में उस विचारधारा का ध्वजावाहक था जिसके अशोक चक्रधर कार्यकर्त्ता थे। अशोक चक्रधर ने लिखा ही है, "दरअसल, उस समय वैचारिक रेखाएँ इतनी तीखी और अलगाव करने वाली होती थीं कि जैसे एक परिवार में बाँट लिया जाए कि चाचा तेरा ताऊ मेरा, बुआ तेरी मौसी मेरी।"
बात 1983 की है। अशोक चक्रधर ने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था और नंदन जी ने मुझे उसके प्रीमियर की रिपोर्टिंग के लिए भेजा था। तब मैंने 'दिनमान' में रिपोर्टिंग करते हुए लिखा था। मैं विशेष उत्साह के साथ नहीं गया था। परसाई की पाठशाला का शिष्य, मैं, सीता अपहरण केस नामक व्यंग्य लिख चुका था और इस मूड में 'पंगु गिरि लंबै' पढ़ते ही लगा था कि फिल्म भक्तिभाव से भरपूर होगी। जब रीगल के दरवाजे पर महिलाओं को हाल में जाने की प्रतीक्षा में बतियाते देखा तो विश्वास हो गया। जिसकी कृपा से गूँगा बोलने लगता है, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है और लँगड़ा पहाड़ पर चढ़ने लगता है, ऐसे ईश्वरीय चमत्कारों पर अपनी कभी भी आस्था नहीं रही है। अपन मजाक के मूड में बैठे थे। अपने समय में घोर प्रगतिशीली कार्यकर्ता रहे अशोक चकधर के भक्तिभाव को भी देख लिया जाए। पर मन सावधान भी कर रहा था कि अशोक चक्रधर को लेकर इतने पूर्वाग्रही मत हो जाओ।
वृत्तचित्र के बारे में आम दर्शकों की प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग हो सकती हैं, परंतु उनका निष्कर्ष एक ही रहता है- समय और धन की बर्बादी कुछ इसे समय और सरकारी पैसे की बरबादी मानते हैं तो कुछ इसे अन्य सरकारी सूत्रों की तरह जबरदस्ती दिया गया प्रसाद मानते हैं। कुछ इसे फिल्म शुरू होने से पहले अँधेरे में आँखें सेट करने का सिलसिला कहते हैं और कुछ इसे भारतीय परंपराओं का पालन करते हुए देर से आने वाले दर्शकों के लिए वरदान कहते हैं। आम दर्शक का निष्कर्ष यही है कि वृत्तचित्र नीरस, उबाऊ आँकड़ेबाज, सरकारी ढोल पीटनेवाला तथा फिजूल होता है। 'पंगु गिरि लंबै' का निमंत्रण मिलने पर जब मैंने अपने एक दर्शक मित्र से कहा, 'चल रहा है फिल्म प्रीमियर देखने' तो मैं उसका सच्चा मित्र सिद्ध हो गया और वह मेरे अहसानों से दब गया। परंतु जब मैंने उसे बताया कि मैं उसे पंद्रह मिनट की डॉक्युमेंटरी दिखाने ले जा रहा हूँ तो उसका मुँह कड़वा हो गया और उसने अहसान का सारा बोझ मेरे कंधे पर लौटाते हुए कहा, 'तू दस रुपए साथ दे तो भी न चलूँ, समझा। मैं क्या फालतू हूँ।'
परंतु 'पंगु गिरि लंघु' ने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। ईश्वर पर तो नहीं मनुष्य की शक्ति पर आस्था बढ़ गई। अशोक चक्रधर और दुलाल साइकिया द्वारा 'गतिचित्रम्' के बैनर के अंतर्गत बने इस वृत्तचित्र में एक नए कोण और भिन्न तरीके से चीजों को देखा गया है। आदमी आदमी का भाग्य बदल सकता है। ऐसे अपंग बैसाखियाँ जिनकी जिंदगी ढो रही थीं, उन्हें अपने पैरों पर अपने सहारे खड़ा करने का अद्भुत कार्य किया है- सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र ने यहाँ के डॉ० पी०के० सेठी, डॉ० कासलीवाल तथा शिल्पकार मास्टर जी की अथक कल्पना और प्रयत्नों ने अपंगों को बैसाखियों के सहारे नहीं 'कृत्रिम परंतु प्राकृतिक पैर की तरह गतिवान अपने धरातल पर खड़े होने की शक्ति दी है। उन्होंने इस देश की जरूरतों के अनुसार कृत्रिम पैर बनाए हैं, इस पैर को लगाकर चलना, दौड़ना, उकड़ू बैठना, पालथी मारना, चढ़ना, कूदना, तैरना सब संभव है। अब तक हम पश्चिमी देशों के अनुरूप भूनाए गए पैरों मात्र पर ही खड़े थे। अब हम अपने अनुसार बनाए गए पैरों के द्वारा अपनी धरती पर उठ-बैठ, खा-पी सकते हैं।
अशोक चक्रधर और दुलाल साइकिया ने इस वृत्तचित्र में मात्र कृत्रिम पैर बनाने के कारखाने, आँकड़ों, डाक्टर और शिल्पकार से साक्षात्कार को ही कैमरे में कैद नहीं किया है, अपितु असंख्य रोगियों के चेहरों पर तैरती मानवीय संवेदनाओं को सेल्यूलाइड पर उतार दिया है। वर्षों से जो लोग दूसरों पर बोझ बने थे, वही अब रिक्शा चलाकर दूसरों को ढो रहे हैं। उनके चेहरे पर श्रम और आत्मविश्वास की आई चमक को अशोक और दुलाल ने दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है।
कृत्रिम पैर लगाए एक बच्ची जब हिचकती झूले की ओर बढ़ती है, पाँव झूले पर रखती है। धीरे-धीरे झूले की पेंग बढ़ाने के साथ उसके चेहरे का आत्मविश्वास और मुस्कान बढ़ जाती है, तब दर्शक सम्मोहित हो उठता है, फिल्म समाप्त हो जाती है। पंद्रह मिनट कहाँ गए पता नहीं चलता। सामाजिक उद्देश्य और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने वाला यह वृत्तचित्र अपनी बात रोचक ढंग से कह देता है। अशोक और दुलाल ने वृत्तचित्र की उस परंपरा को तोड़ा है कि वृत्तचित्र को मात्र एक कमेंटरी होना चाहिए। इसमें शिब्बू के छायांकन और पं० शिवप्रसाद के संगीत का विशेष योगदान है। संपादन ने फिल्म को तीव्रता दी है और अनावश्यक विस्तार से बचाया है।
फिल्म समाप्त होने से अशोक चक्रधर संतुष्ट नजर आ रहे थे। परंतु जब मैंने पूछा कि फाइनेंस की क्या और कैसे व्यवस्था की तो उनकी संतुष्टि गायब हो गई, बोले, "भई अभी तो गाँठ का पैसा लगा दिया है। कुछ युनाइटेड बैंक से कर्ज लिया है, कुछ दोस्तों की जेब हल्की की है। अस्सी हजार रुपए इस प्रोजेक्ट में लग गए। अब देखो अगर फिल्म डिवीजन वाले खरीद लें तो बात बने। कीटाणु तो बहुत देर से कुलबुला रहे थे। बहुत पहले अपनी कविता 'बूढ़े बच्चे' पर फिल्म बनाने की सोची थी। मैं केवल सूचनात्मक उबाऊ फिल्म नहीं बनाना चाहता था, उसे सामाजिक उद्देश्य और मानवीय संवेदना के साथ जोड़ना चाहता था। बस कूद पड़ा मैदान में मार्च '83 के अंत में आइडिया बना और अप्रैल में चार दिन में हमने शूटिंग कर डाली। मई से लेकर अगस्त तक के चार महीनों ने कई खिड़कियाँ मेरे सामने खोलीं। रिफ्लेक्टर उठाने से लेकर निर्देशन तक का अनुभव प्राप्त किया।"
अशोक चक्रधर कुछ न कुछ नया रचने में विश्वास रखते हैं। उनके अंदर रचनात्मक ऊर्जावान एक बच्चा है जो निष्क्रिय नहीं बैठ सकता। यह बच्चा आपको भी उकसा सकता है। आप उकस गए तो ठीक अन्यथा वो तो कुछ न कुछ रचेगा ही। यह हमारे विकसित संबंधों का ही परिणाम था कि पद्य और गद्य व्यंग्य की एक जैसी पर अलग-अलग नाव के मल्लाह अक्सर एक दूसरे से साहित्य की नदी में मिलते रहते। लेखक होने के कारण मेरे कॉलेज के प्रधानाचार्य, मेरे दोस्त राजेंद्र पंवार मुझे हास्य व्यंग्य का कवि ही मानते थे। उनका विश्वास था कि सुरेंद्र शर्मा, गोविंद व्यास, अशोक चक्रधर मेरे खास दोस्त हैं और मेरे एक बार कहने पर केवल टैक्सी के भाड़े में आ जाएँगे। वैसे गोविंद व्यास और सुरेंद्र शर्मा उनके भी कम दोस्त नहीं थे। अशोक चक्रधर अनेक बार मेरे कहने पर कॉलेज आए और कभी भी अतिरिक्त माँग नहीं की। मुझे जब भी आवश्यकता हुई, अशोक चक्रधर भाई, बिना न नुकुर के हाजिर मिले और जब अशोक भाई ने कोई आग्रह किया तो मेरा भी न नुकुर तेल लेने चला गया।
चावल का एक दाना पेश है-
बात 1996 की है। 1984 में मुबई के चकल्लस कवि सम्मेलन का हिस्सा बना था। अगले दिन भारती जी से मिला और उन्होंने जो सलाह दी उसके बाद कवि सम्मेलनों का मोह छोड़ दिया था। वैसे भी मेरा परसाई शिक्षित व्यंग्यकार मन, कवि सम्मेलनीय हास्य से बिदकने लगा था। मुझे अशोक चक्रधर भाई के कलात्मक लेटर हैड पर लिखा एक पत्र मिला। यह पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित है। इस पत्र पर 20 नवंबर 1996 की तिथि अंकित है। लिफाफा क्या पेश करूँ, पूरा मजूमन ही लिख देता हूँ। पत्र का मजमून था--
30 नवंबर 1996
डियर प्रेम बाबू,
दिनांक 29 नवंबर से 'फुलझड़ी एकस्प्रेस' नामक एक हास्य-व्यंग्य कवि सम्मेलन - मुशायरा धारावाहिक, डी डी -1 राष्ट्रीय प्रसारण में हर सप्ताह रात्रि 10.30 पर प्रसारित होने रहा है। चार ऐपीसोड की रिकार्डिंग संपन्न हो चुकी है।
पहली बात तो यह कि आप कृपया 'फुलझड़ी एकस्प्रेस' देखें और अपनी राय बताएँ। दूसरी यह कि हास्य-व्यंग्य, तंजो-मिजाह की जानी मानी हस्ती होने के नाते आप भी इस कार्यक्रम में भागीदारी करें- ऐसी मेरी कामना है। अगली रिकार्डिंग बहुत शीघ्र होने जा रही है।
यह कार्यक्रम सी०पी०सी० की निदेशिका श्रीमती कमलिनी दत्त की परिकल्पना है एवं इसका निर्माण सी०पी०सी० दूरदर्शन केंद्र के एक सुयोग्य प्रोड्यूसर श्री सुरेंद्र शर्मा कर रहे है। फिलहाल मुझे इस कार्यक्रम के संचालन का कार्यभार सौंपा गया है।
स्वस्थ और निर्मल हास्य की दो-तीन रचनाएँ आप मुझे तत्काल भेज दें। इससे कार्यक्रम को अच्छी तरह पेश करने में आसानी रहेगी। फुलझड़ी एक्सप्रेस के हर ऐपीसोड में संचालक समेत कुल छह कवि-शायर रहते हैं। प्रत्येक के हिस्से में लगभग चार मिनट का समय आता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी रचनाओं का चयन करें।
मुझे आपकी रचनाओं का बेकरारी से इंतजार रहेगा। अपनी कविताएँ, गज़लें, कृतांत मुक्तक, गीत अथवा निबंध आप मुझे मेरे निवास के पते पर भेजें। यदि चाहे तो 6944040 पर फैक्स द्वारा भी भेज सकते हैं। मीडिया की सीमाओं एवं शक्तियों से आप अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए रचनाओं को चुनते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी रचनाओं को देश के सर्वश्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य-लेखन का उदाहरण बनना है।
मेरी भूमिका महज एक प्रस्तावक की है। मैं आशा करता हूँ कि दूरदर्शन की ओर आपको शीघ्र ही विधिवत निमंत्रित किया जाएगा।
यह पत्र मैं ज्यों का-त्यों अपने सभी सूचीबद्ध कवि और शायर साहेबान को भेज रहा हूँ। इसलिए इसकी भाषा यदि आपको थोड़ी औपचारिक लगे तो क्षमा कर दीजिएगा।
नमस्कार सहित-
अशोक चक्रधर"
समझदारों को इस पत्र द्वारा आत्मीय मित्रों के प्रति अशोक चक्रधर भाई का सहज भाव समझ आ गया होगा। अशोक भाई जितना अपने सम्मान के प्रति सजग हैं उतने ही अपने आत्मीयों के सम्मान के प्रति भी औपचारिक भी होते हैं तो उसका कारण भी रेखांकित कर देते हैं। बहुत कठिन होता है अनौपचारिकों से औपचारिक होना।
मन 'व्यंग्य यात्रा' का चौथा अंक "व्यंग्य कविता हाशिए पर क्यों" पर प्लान किया था। इसका मूल था कि मंच की हास्य व्यंग्य कविता ही व्यंग्य कविता को हाशिए पर धकेलने की दोषी है। अशोक भाई मंचीय कविता के प्रति मेरे संतुलित विरोध को जानते थे। वे यह भी जानते थे कि व्यंग्य यात्रा खुली सोच का मंच है। इसलिए मैंने जब उनसे लिखने के लिए आग्रह किया तो उन्होंने तत्काल एक आलेख 'प्रसिद्धि का प्रसाद' भेज दिया। उस पत्र में अशोक चक्रधर ने इस विषय पर अपनी मान्यता को बिना किसी लाग लपेट के बेबाक लिखा था- प्रसिद्धि का प्रसाद हर किसी को नहीं मिल पाता। जिनको मिलता है वे अचानक समझ नहीं पाते कि कैसे मिल गया। जिनको नहीं मिलता वे कुंठित हो जाते हैं कि क्यों नहीं मिला। सोचते नहीं हैं। कि कैसे नहीं मिला। अब तो इन नवोदित कवियों की संख्या गुणात्मक तरीके से बढ़ रही है। कहाँ हैं वे लोग जो इनसे संवाद करें? मंच पर जाने वाले कवियों के पास क्या इतना समय है कि मंच पर आने की कामना रखने वाले इन कवियों को मंच पदार्पणपूर्व संवाद का एक मंच प्रदान कर सकें। तथाकथित महान साहित्यकार मंच की कविता को कविता मानते ही नहीं हैं। उनसे बहस में नहीं उलझना चाहता। मंच की कविता को पूर्ण कविता मैं भी नहीं मानता, लेकिन जिसे वे पूर्ण कविता सिद्ध करना चाहते हैं वह पूर्ण कविता हो ये भी नहीं मानता। शास्त्रीय कविता सार्वकालिक होती है। हर युग में याद की जाती है। उसकी सरलता या जटिलता मायने नहीं रखती, मायने यह बात रखती है कि उसका अपने युग और जीवन से कितना सरोकार है। दूसरी बात, हंसाना कोई पाप तो नहीं। साहित्यकारों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो हंसाने वाले काव्यात्मक प्रयत्नों को काव्य के घेरे में घुसने ही नहीं देता। चलिए, उनसे भी कैसा शिकवा।
इस समय समस्या तो ये है कि तुकबंदी अथवा बंदतुकी के अनेक प्रकारों में स्वयं को कविता के रूप में पहचाने जाने के लिए जो फसल दिख रही है उसके लिए क्या किया जाए? खाद कहाँ से लाई जाए? पानी कहाँ से जुटाया जाए? खरपतवार कैसे निकाली जाए? कविता की वालियों को भ्रांतिमान अलंकारों के टिड्डों से कैसे बचाया जाए? बाजारवादी इस युग में उसकी पैठ कहाँ लगे? आढ़तियों के बिना गुजारा भी नहीं है, पर कविता के गल्लेबाजों से नए किसानों के हितों की रक्षा कैसे की जाए।"
किसने कहा, क्यों कहा और कब कहा मैं नहीं जानता, पर कहा ज़रूर है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे डुबाने वाले दो तरह के होते हैं। एक इस तरह डुबाते हैं कि साँसे रुक जाती हैं और जीवन की धड़कन मुर्दा हो जाती है। दूसरी तरह के डुबाने वाले अपने में इस तरह डुबोते हैं कि आप उनके साथ तैरते हुए किसी अच्छे तैराक जैसा आनंद लेते हैं। बिहारी ने भी तो ऐसों-जैसों के लिए कुछ कहा है न- ज्यों ज्यों बूढे श्याम रंग, त्यों त्यों उजलो होई। तो अशोक चक्रधर खुद तो कर्मक्षेत्र में डूबे बिना चैन नहीं लेते हैं और न दूसरे को लेने देते हैं। न्यूयार्क में संपन्न हुए आँठवें विश्व हिंदी सम्मेलन से अशोक चक्रधर लौटे तो वहाँ हिंदी कम्प्यूटिंग में लगी हुई टीम संग उन्होंने फैसला किया कि हिंदी साहित्यकारों और हिंदी प्रेमियों के बीच आंकिक विभाजन को समाप्त करने के लिए और कंप्यूटर चेतना का विकास करने के लिए 'हिंदी का भविष्य और भविष्य की हिंदी' शीर्षक से प्रतिमास एक मासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इधर सोचा और उधर सितंबर 2007 से जयजयवंती संगोष्ठी के कार्यक्रम आरंभ हो गए। हर कार्यक्रम में कंप्यूटर से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया। गंभीर चर्चाओं के दौरान काव्य पाठ भी होते रहे। संचालन के दौरान अशोक चक्रधर प्रायः कहते रहे कि हमारा कार्यक्रम रोचक संप्रदाय का भी है और भौंचक संप्रदाय का भी है। कविताओं और रचनात्मक साहित्य की विविध विधाओं से हम इसे रोचक बनाते हैं और भविष्य की हिंदी के लिए कंप्यूटर की सेवाएँ देखकर भौंचक भी रह जाते है। हमारा मकसद है कंप्यूटर का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए स्वयं को सक्षम बनाना। इस मासिक गोष्ठी में जिस वरिष्ठ साहित्यकार को 'जयजयवंती सम्मान' से सम्मानित किया जाता उसे हिंदी सॉफ्टवेयर सुविधा सज्जित एक लैपटॉप भी दिया जाता। (मेरे पास पहले से ही कंप्यूटर था और मैं बहुत कुछ कंप्यूटर योग्य था अतः मुझे इस सम्मान के योग्य नहीं समझा गया।)
अशोक चक्रधर के अंदर एक सकारात्मक सोच का वह इंसान बैठा है जो अपना क्या दूसरे का शोक पसंद नहीं करता है, शोक से उबरना/उबारना पसंद करता है। यह इंसान आपको शोक में डूबा देखकर अपना शोक भूल जाता है। उसके पास आपको दिलासा देने वाले शब्दों का कोश है। एक ऐसी ही याद जो मेरे अविस्मरणीय यादों के कोष का हिस्सा है, उसे साझा करना चाहता हूँ।
बात 2014 की है, जुलाई 24 की। केंद्रीय साहित्य अकादेमी के सौजन्य से साहित्यकारों का प्रतिनिधि मंडल, सात दिवसीय दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के लिए रवाना हुआ । इस यात्रा का उद्देश्य था - भारतीय उच्चायोग एवं हिंदी शिक्षण संघ द्वारा आयोजित हिंदी साहित्य सर्वश्री नरेश सक्सेना, अशोक समारोह में भाग लेना। इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे चक्रधर, ओम निश्चल, प्रेमशंकर शुक्ल, शिवनारायण, भगवान सिंह और मैं (इस यात्रा के साथ जुड़ी अनेक सुखद स्मृतियाँ हैं, जिनकी चर्चा करने लगूँगा तो इसीमें खो जाऊँगा और विषयांतर कष्टदायक होगा।) मुझे 26 जुलाई को आयोजित सत्र में 'इक्कीसवीं सदी के नए आयाम' सत्र में 'इक्कीसवीं सदी में व्यंग्य' पर अपनी बात कहनी थी। विदेशों में हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर मेरे अधिकांश अनुभव त्रिनिदाद के थे जो उत्साहवर्धक नहीं थे। और यहाँ तो हिंदी व्यंग्य की इक्कीसवीं सदी पर कहना था। पर मुझ आश्चर्य हुआ कि न केवल कार्यक्रम में प्रबुद्ध श्रोता थे अपितु वहाँ के निवासी शिवाजी श्रीवास्तव और विनय सिंह ने अपनी बात कही और मुझसे सवाल भी किए। दक्षिण अफ्रीका में व्यंग्य विमर्श मुझे हर्ष दे गया। दक्षिण अफ्रीका में अनेक घटनाओं ने हर्ष दिया, पर दक्षिण अफ्रीका के विदाकाल ने एक ऐसा दुखद समाचार दिया जिसने मुझे तोड़ दिया। अब भी उस समाचार को याद करता हूँ तो दक्षिण अफ्रीका की सुखद स्मृतियाँ कष्ट में परिवर्तित होने लगती हैं। जैसे समुद्र किनारे रेत से बनाई, संपूर्ण होने की दिशा में, कलाकृति को समुद्र की एक लहर दुखद अंत दे देती है।
बात 30 जुलाई की है। दक्षिण अफ्रीका से हमारी विदाई का दिन था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त श्री वीरेंद्र गुप्ता ने अपने निवास पर कवि सम्मेलन संग रात्रि भोज का आयोजन किया था। जमीन से जुड़े श्री वीरेंद्र गुप्ता का आतिथ्य गजब का होता है। ऐसे समय में वे केवल मेजबान होते है और उच्चायुक्त पद से स्वयं को मुक्त कर अतिथियों की देखभाल करते हैं। उनकी पत्नी वीणू गुप्ता उनका पूरा साथ देती हैं। उनके साथ त्रिनिदाद और टोबैगो में काम करते हुए जुड़ाव की अनेक सुखद स्मृतियाँ हैं। उनके साथ हुआ जुड़ाव आज भी पारिवारिक धरातल पर प्रगाढ़ हो रहा है।
हम लोग बहुत दिनों बाद मिले थे अतः बहुत-सी बातें उनके और वीणू के साथ बाँटने की थीं। आत्मीय क्षणों से सराबोर सब सुखद चल रहा था कि दिल्ली से फोन आया। यह पहली बार नहीं थी कि मेरे दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान दिल्ली से फोन आया हो। यात्रा आरंभ करने से पूर्व मेरे बड़े बेटे ने वहाँ का सिम कार्ड मेरे फोन में डलवा दिया था। इसका प्रयोग मेरे अन्य सहयात्रियों ने भी किया। लगभग प्रतिदिन मेरा हालचाल जानने को वे फोन कर ही लिया करते थे। और फिर यह तो विदा की शाम थी। मुझे लगा कि औपचारिक-सा फोन होगा। मेरी पत्नी को पता है कि 30 की शाम वीरेंद्र गुप्ता के यहाँ होऊँगा और वीणू गुप्ता से बात करने को उसने फोन किया होगा। पर यह मेरी पत्नी का नहीं मेरी बहु अभिलाषा का फोन था। वह बहुत हिम्मतवाली है, धैर्य कम ही खोती है। अभिलाषा ने जिस तरह चुप्पी के बाद टूटती एवं दुखद आवाज के साथ फोन आरंभ किया, आशंकित मन थरथरा उठा। अभिलाषा ने सूचित किया कि पंचकूला निवासी मेरे छोटे भाई सत्य प्रकाश कुंद्रा, जिसे हम घर में कुक्कु नाम से पुकारते थे, हृदयगति रुकने से निधन हो गया है। मैं एकदम सन्न रह गया। आयोजित आयोजन अपने उच्चायोगीय रंगत में रंगा चढ़ाव पर था। मैं चुपचाप खिसकता हुआ, फोन सुनने की प्रक्रिया में बाहर निकल गया। मेरी पत्नी आशा बेटा-बहू पंचकूला के रास्ते में थे और मुझे बहुत कुछ समझा रहे थे पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों ओर जैसे एक शून्य तैर रहा था । रुदन मेरे अंदर फूट रहा था। विवशता इतने विकराल रूप में मेरे समक्ष आएगी कभी सोचा न था। मैं अनेक सवालों से जूझने भी लगा। क्या उसके अंतिम दर्शन तक न कर पाऊँगा, कैसे बीतेंगे एक-एक क्षण! कल की फ्लाइट से तो निकलना ही है पर क्या अभी कोई फलाईट लेकर उड़ूँ... पार्टी छोड़कर चला जाऊँ... और बहुत कुछ? तभी मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। मुड़कर देखा तो यह हाथ अशोक चक्रधर का था।
- क्या हुआ कुछ अनिष्ट घटा है क्या?
- नहीं ... कुछ नहीं....
- कुछ नहीं, बहुत कुछ है प्रेम डियर! तुम्हारा चेहरा बता रहा है.....
जिससे चेहरा न छुपा सकें उसे सब कुछ बताना ही पड़ता है और मैंने भी बताया। अशोक भाई ने कहा- यह तुम्हारा वही भाई है न जो हरियाणा टूरिज़्म में था! इसीके बुलाने पर हम सब चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में गए थे न! दो महीने पहले ही तो आई०आई०सी० में तुम्हारी सेवा निवृत्ति वाली पार्टी में मिला था।" अशोक चक्रधर की स्मृति अद्भुत है। दूसरे की हर भूली दास्तान उन्हें याद रहती है। सही कहा था अशोक भाई ने कि मेरा यह वही भाई था जिसने लो बजट पर कवि सम्मेलन आयोजित करने की चिंता को दूर करते हुए अपने कार्यालय में कह दिया था कि अशोक चक्रधर मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं और इतने कम में भी आ जाएँगे। मैंने अशोक भाई को अपने भाई का यह विश्वास बताया तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा छोटा भाई है न प्रेम डियर तो भाई तो अपना भी छोटा भाई हुआ। मेरा यह वही भाई था जिसने दो माह पूर्व कॉलेज से मेरी सेवा निवृत्ति के आयोजन पर आए अशोक चक्रधर से अपने परिवार संग चित्र खिंचवाने के लिए कहा तो अशोक चक्रधर, किसी से की जा रही महत्त्वपूर्ण बात को बीच में छोड़कर मुस्कराते हुए आ गए थे।
अपने छोटे भाई के एक दर्दनाक कष्ट को अशोक चक्रधर भी भोग चुके थे। उस दिन अशोक भाई ने 'शो मस्ट गो ऑन टाईप से उपजा कष्ट मुझसे साझा किया। मित्र ने जो शब्द कहे वे कोरे शब्द न थे, उनसे संवेदना बरस रही थी। अशोक भाई ने बताया कि वे भी अपने छोटे भाई के भंयकर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मरणासन्न स्थिति के कारण किंकर्तव्यमूढ़ स्थिति झेल चुके हैं। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैं और किसी से कुछ न कहूँ, बस वीरेंद्र गुप्ता के साथ समाचार साझा कर दूँ और सामान्य दिखता हुआ वापस पार्टी में चलूँ। भुक्तभोगी जानते होंगे कि ऐसे सामान्य दिखना कितना कठिन है। पर जब अशोक चक्रधर जैसा साथ हो तो कठिनाई सरल हो जाती है। उस दिन भी भारी समय बहुत कुछ हल्का हुआ।
मैंने श्री वीरेंद्र गुप्ता को बताया। विदेश सेवा में रहते वे ऐसी अनेक दुर्घटनाएँ झेल चुके थे। उन्होंने न केवल गीता पढ़ी थी अपितु उसे अनेक बार व्यवहार में लाना भी पड़ा था। उन्होंने जो कहा वह ज़मीनी हकीकत से जुड़ा था। वे जानते थे कि मैं परिवार को लेकर कितना संवदेनशील हूँ। अपने पिता के एक बार कहने पर कि अब तू आ जा प्रेम, मैं 2002 में त्रिनिदाद में एक वर्ष और रुकने के 'लालच' को त्याग आया था। श्री वीरेंद्र गुप्ता ने अंतिम निर्णय मुझ पर छोड़ दिया। अशोक भाई और वीरेंद्र गुप्ता जी का ज्ञान मेरे पास था और अब कर्म मुझे करना था। मैंने उनके ज्ञान को धारण किया और जीवन की कष्टदायक यथार्थ का सामान्य होकर सामना करने लगा। मैंने दोनों से आग्रह किया कि वे किसी अन्य से इस दुखद प्रसंग की चर्चा न करें। होटल के कमरे में मेरे सहभागी रहे मेरे मित्र ने मेरी उदासी पकड़ी और आत्मीयता से कारण पूछा। इन सात दिनों में वे मेरे आत्मीय बन चुके थे। मैंने उन्हें इस कारण बता दिया कि कहीं वे बाद में शिकायत न करें कि मैंने उन्हें पराया समझा। उन्हें बताया तो उन्होंने संवेदना प्रकट की। मेरे भाई को वह जानते नहीं थे अतः और क्या प्रकट करते। मेरे लिए यही बहुत था।
अशोक चक्रधर भाई, केवल संबोधन के भाई न होकर एक अभिभावक की तरह पूरी यात्रा मेरे साथ रहे। दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली तक की वाया मुंबई, यात्रा बहुत लंबी थी और उस दिन तो इसे मेरे लिए अनेक गुणा लंबा होना था। अशोक भाई इस लंबे कठिन समय को अपने विशद अनुभव साझा करते हुए, छोटा करते रहे। उन्होंने इस दुखद प्रसंग को बहुत बाद में, श्री नरेश सक्सेना जी से साझा किया था। विदा होते हुए नरेश सक्सेना जी की नम आँखें और मेरे कंधे पर पड़ा हाथ बहुत कुछ कह रहा था।
उस दिन अशोक चक्रधर जी से विदा लेते हुए मैंने महसूस किया कि दूसरों को हंसाने वाले इस व्यक्ति के अंदर करुणा का कितना समृद्ध कोष है। अशोक भाई को जो सज्जन/दुर्जन बहुत समीप से जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि ज़माने की तोताचश्मी ने उन्हें कितने आघात दिए हैं। फोन पर हम दोनों किसी प्रेमी प्रेमिका से बतरस का आनंद उठाते हैं। अक्सर हमारे फोन 57 मिनट 57 सेकेंड अवधि के लिए व्यस्त रहते हैं। ऐसी ही हम दो वैष्णवन की वार्ता में अशोक भाई ने अपने अंतस्थल में झांकने का मुझे अवसर प्रदान किया है। अशोक भाई के साथ अकेले में जो कुछ मुलाकातें हुई हैं वहाँ बातों-बातों में कुछ दर्द भी छलके हैं। ऐसी ही मुलाकातों में ज्ञान मिला है कि अनेक के आँसू पोंछने वाले अशोक ने स्वयं भी ऐसे शोक के दुखदायी पल बिताएँ हैं जब उसके आँसूओं को कोई देखने वाला नहीं था। निश्चित ही इस वाक्य को पढ़कर सबके अपने-अपने आँसू छलके होगें संसार ऐसा ही है कि शैली में दार्शनिक होकर कहा जा सकता है कि ऐसा कौन है जिसके दूसरे की बेदर्दी कारण आँसू न निकले हों और... और ऐसा कौन है जिसकी बेदर्दी ने दूसरे के आँसू न निकाले हों।
कड़की के दिन थे। पाँच बंडल बीड़ी लेकर उसके टोटो तक पीने वाले दिन। खाना मिला तो खाया नहीं तो कोई व्रत रखने का संतोष मनाया। कड़की के इन्हीं दिनों में पार्टी के इस कार्यकर्ता से निर्देशात्मक आग्रह किया गया कि परहित भाव जगाओ और लगने वाली अपनी नौकरी पर किसी अन्य की सिफारिश ले जाकर उसे जमाओ। हे जनता! मैदान खाली करो। कार्यकर्ता मन ने समझाया कि अग्रज हैं और नए-नए पार्टी में आए हैं, तू त्यागी बन ही जा पर त्यागी बन अपने स्थान पर जिस दूसरे को प्राध्यापक लगाने का आग्रह किया और नौकरी लगने पर जब बधाई देने घर गए तो उपेक्षा के ऐसे कोड़े बरसे कि सशक्त हृदय भी आँसुओं को न रोक सका। मिठाई तो दूर मीठे पानी की दो बूंद भी नसीब नहीं हुई। हँसी को अपनी कलम का हिस्सा बनाने वाले कवि मन की आँखों से बरबस आँसू बरस गए। ऐसे ही पाँच बंडल बीड़ी और एक समय के भोजन की व्यवस्था के लिए अपनी कलम जिस प्रकाशक को बेची उसने काम के बदले अनाज का शगुन तो क्या देना था, 'अशोक' को भिक्षुक मान, टरकाऊ शैली में कहा - फिर आना। दो सौ रुपए की अपेक्षा से गए लेखक को दो फूटी कौड़ी न मिली। ढाबे वाले से लेकर बीड़ी वाले का उधार चुकाने के संकल्प से गए मन से आँसू तो बरसने ही थे।
मेरे पास अशोक चक्रधर से जुड़ी स्मृतियों का एक समृद्ध कोष है। इस कोष में नवरस-सा रशियन क्लचरल सेंटर है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में गुजारी शामें हैबिटेट सेंटर की कर्मस्थली है, त्रिनिदाद की दोबारी यात्रा, मॉरिशस का विश्व हिंदी सम्मेलन, 'गगनाचंल' का मेरा संपादन, अशोक की पीठ पीछे किए गए मिथ्या वार हैं, हिंदी अकादमी दिल्ली और केंद्रीय हिंदी संस्थान का उनका उपाध्यक्ष पद प्यारी नेहा है, बागेश्वरी है... इन सब रसों पर एक एक अध्याय भी लिखूँ तो महा उपन्यास बन जाएगा। जिस अल्पबुद्धि लेखक ने व्यंग्य उपन्यास न लिखा हो वह महा उपन्यास क्या खाकर लिखेगा। इसलिए अभी इतना ही।
- प्रेम जनमेजय की स्मृति से
| व्हाट्सएप शेयर |
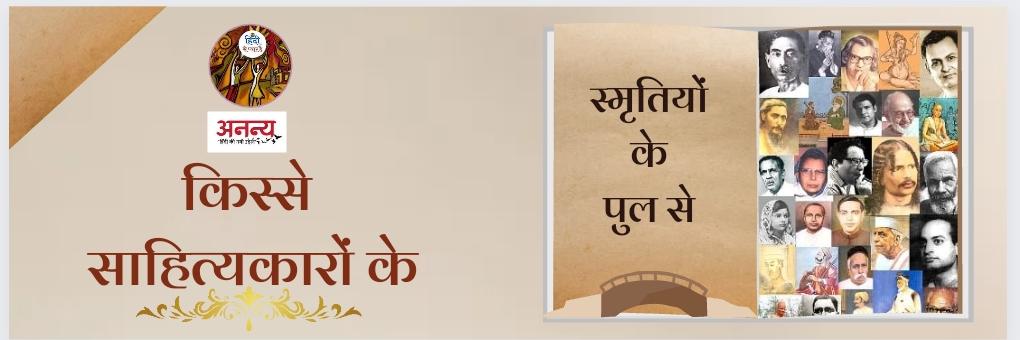
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें