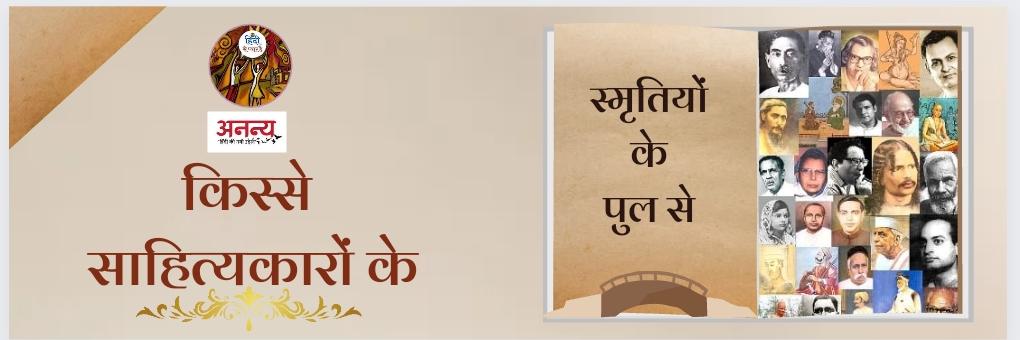अज्ञेय- नागर जी आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करना चाहता हूँ।
आप शायद पहले ही दो-चार सवालों से सोचेंगे, क्या बेवकूफी के सवाल हैं, इनके जवाब तो मालूम होने चाहिए ! लेकिन कुछ
सवाल इसलिए पूछूंगा कि आपके मुंह से उनका जवाब मिल जाये 'ताकि सनद रहे और वक्त
जरूरत काम आये'। पहले तो यह
बतायें कि आपने लिखना कब शुरू किया और सबसे पहली क्या रचना थी ?
नागर -फूटी पहले तुकबंदी। तुकबंदी फूटी जब १९२८-२९
में साइमन कमीशन गो बैक' का जुलूस निकला
था। बड़ा विशाल जुलूस था- कान्यकुब्ज कॉलेज, रेडियो से, स्टेशन रोड से सिटी आते हुए उसी में दबा-कुचला मैं भी। उस
पर लाठी चार्ज हुआ था, जवाहरलालजी और पंडित गोविंदबल्लभ पंत पर। लोग पीछे हट रहे
थे। पीछे वालों को पता नहीं था कि आगे क्या हुआ ? बीच में मैं- बहुत दबा-कुचला। वहां से लौट कर
फिर आवेश में पहले जो फूटी वह तुकबंदी थी। लेकिन उसके साथ-ही-साथ एक बात अच्छी याद
से आपको बतला सकता हूं कि गद्य लिखने की रुझान मेरी लगभग १९२७-२८ में छोटी उम्र से
हो चली थी। तुकबंदी एक तो शायद इसलिए फूटी कि माहौल जो था उस समय लखनऊ में या तो
शेरो-शायरी की बैठकों का था या कवि-गोष्ठियों का था। कविता इसलिए फूट पड़ी।
आश्चर्य यह स्वयं मुझे भी होता है कि एकाएक कविता क्यों फूट पड़ी जबकि प्रोज भी
लिखता था।
अज्ञेय : फिर आपने और भी छंद लिखे या कि...
नागर थोड़े से लिखे। बाद में पैरोडी करने लगा। 'चकल्लस' में पैरोडी काफी की -
प्रसादजी के आंसू की की, हितैषीजी की की, सोहनलाल द्विवेदी के 'किसान' की की, बहुत-सी कीं। फिर कविता
करने की रुचि जो थी वह समाप्त हो गयी। पर तब अकस्मात् तुकबंदी ही क्यों फूटी, कह नहीं सकता।
अज्ञेय : फिर गद्य में शुरू में कहानी लिखी या कि
उपन्यास से ही आरंभ किया ?
नागर - शुरू में कहानी, कहानियां लगभग '२९-३० से ही लिखीं, लेकिन छपी नहीं। छपने के
नाम पर यह होता कि वापसी के लिए भेजे गये टिकट भी कभी-कभी वापस मिलते थे, कभी तो टिकट भी गायब हो
जाते थे। शुरू में मैंने उपन्यास नहीं लिखा था हालांकि उपन्यास उस जमाने में पढ़े
खूब थे। एक चीज और है। अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ने का चाव मुझे क्रिश्चियन कॉलेज
में आ कर लगा सन् '३३-३४ में।
अज्ञेय : आपको याद है, जो उपन्यास आपने तब पढ़े उनमें से कौन से आपको अच्छे लगे ?
नागर - शुरू तो किया था मोपासां की कहानियों से। बाद
में उनकी पांच-छः कहानियों के अनुवाद भी किये। फिर लाबर का 'मदाम बोवारी' पढ़ा, उसका भी अनुवाद किया।
बाल्जाक का उपन्यास पढ़ा था- बड़ा अच्छा उपन्यास था, ३-४ पढ़े। अलेक्जेंडर ड्यूमा भी पढ़े। बाद में
दोस्तोएव्स्की के पढ़े। के तोल्स्तोय के और भी बाद में पढ़े। चेखोव की कहानियां
पढ़ी; उनका भी अनुवाद
किया था।
अज्ञेय : ये जो अनुवाद आपने किये, ये मूल रचना के प्रति
आकर्षण के कारण, या अनुवाद करना
था किसी चीज के पारिश्रमिक के लिए।
नागर : भाई, दो बातें थीं मन में। शुरू में कहानी लिखने की जो लहर चली
उसमें बाहर से कोई चीज छू गयी तो कहानी लिख डाली। कभी-कभी चंडीप्रसाद मिश्र 'हृदयेश' और प्रसादजी की शैली का
नशा चढ़ जाता तो उस टाइप की लिख डाली। फिर मन में यह लगा कालेज में आते-आते कि नहीं, कहानी लिखनी है तो पढ़ो।
जब पढ़ा तब यह हुआ कि उनका अनुवाद करो: अनुवाद करने के बहाने तुम खाली भाषा के ऊपर
ध्यान दोगे, प्लाट तो है ही
सामने, देखो कहानी कैसे
चल रही है। यह साल-डेढ़ साल किया। कहानी के वर्ल्ड मास्टर पीसेज का संग्रह है— दस
जिल्दों में-उसमें से भी बहुत-सी कहानियां लीं। दो छपीं भी। मोपासा की कुछ
कहानियां अनुवाद कीं, वे छप गयीं। फिर
एक संग्रह निकल गया। चेखोव की कहानियां 'काला पुरोहित' के नाम से पुस्तक मंदिर ने छापीं। तो अनुवाद मूलतः इसलिए
किये थे कि हाथ बैठ जाय-किसी आग्रह से नहीं किया।
अज्ञेय : आपकी पहली रचना कौन-सी छपी, जिससे आप मानेंगे कि आपका
साहित्यिक जीवन वास्तव में आरंभ हो गया।
नागर : देखिये, दो कहानियां थीं पास-पास लिखी हुई। एक थी 'प्रायश्चित' - वह हमारे पहले संग्रह में
भी है और एक थी 'अपशकुन'। एक सामाजिक कथा थी उससे प्रेरित हो कर लिखी थी। एक मेरा मित्र अपने घर से भाग
गया था, उसके ऊपर अपशकुन
लिखी थी। संयोग यह हुआ कहानी उस समय हम भेजते थे जहां कहीं भी छप जाये-दिल्ली से
एक पत्रिका निकलती थी 'रंगभूमि', नरोत्तम नागर उसमें बाद
में आये, पहले जो सम्पादक
थे उसके लेखराज ऐसा ही नाम था उसमें 'अपशकुन' पहले छप गयी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि 'प्रायश्चित' पहले लिखी थी। यह
करीब-करीब सन् '३३ की बात है।
अज्ञेय : ये तो अंग्रेजी के या दूसरे विदेशी उपन्यास
आपने बताये। बाकी बांग्ला के या हिन्दी के भी..
नागर - हाँ
बांग्ला के पढ़े।
बंकिम के जो हमारे यहां पुस्तकालय में थे, करीब-करीब सभी
पढ़े। शरत बाबू के, प्रेमचंद के भी पढ़े; जे. पी. श्रीवास्तव पढ़ा, अपूर्णानन्द पढ़ा। 'हिन्दी प्रदीप' की पुरानी फाइल हमको मिल गयी थी, उसमें शुरू में
बालकृष्ण भट्ट के दो तीन अधूरे उपन्यास थे, वे भी पढ़े। 'भारतेन्दु नाटकावली' पूरी पढ़ ली थी। यों काफी पढ़े। हुआ यह भाई, कि बचपन में अकेलापन ५-६
वर्ष की आयु तक रहा। भाई था बहुत छोटा अक्षर ज्ञान जो हमारा उसके बाद घर में जो भी
पढ़ने-लिखने को मिला उसको पढ़ने का चस्का लग गया। पढ़ने के चस्के ने ही अंततोगत्वा
मुझे लेखक बनने की प्रेरणा दी।
अज्ञेय - उर्दू लिपि आप पढ़ते थे या उर्दू के
उपन्यास देवनागरी में....
नागर - उर्दू के उपन्यास देवनागरी में पढ़े। बल्कि कुछ
सुने भी 'तिलिस्म हजूरबा' समय बहुत ही प्रचलित थे।
अज्ञेय - किससे सुने ये उपन्यास या किस्से ?
नागर - एक थे अफीमची, किस्सागो थे पुराने उनसे बहुत से
किस्से सुने। गुलजार मसीम उनसे सुना, जइइश्क उनसे सुना, लगभग साल डेढ़ साल तक उनको अपने पास रखे रहे। वह
सुनाते थे झूम-झूम कर, अजीब तरीके से
सुनाते थे। खातिरदारी उनकी करते थे, चवन्नी रोज, बड़ा अच्छा लगता था उनके कहने का ढंग उर्दू पढ़
नहीं पाये. हालांकि हमारे यहां सेकेंड फार्म में थी।
अज्ञेय: नागरजी, जब हमने-आपने लिखना शुरू किया तब या उससे पहले पढ़ने के लिए
या तो विदेशी उपन्यास थे या बांग्ला का साहित्य था, नहीं तो अधिकतर इसी तरह की चीजें थीं जिसमें
किस्सा प्रधान था - सबसे पहले रोचक कथा होनी चाहिए, और बातें बाद में देखी जायेंगी! आपके अपने
उपन्यासों में यह पक्ष हमेशा काफी सधा हुआ और प्रबल रहा है। क्या आप सोचते हैं कि
जो किस्से आप सुनते रहे उनका यह प्रभाव भी हुआ या कि आप स्वयं ऐसा मानते हैं कि
उपन्यास में सबसे पहली चीज रोचक कहानी होनी चाहिए ?
नागर भाई, सवाल आपका बड़ा अच्छा है। इसका जवाब दो-तीन स्टेज में
दूंगा। पहली यह कि किस्सा सुनने का प्रभाव और उसकी रोचकता मन में कहीं चुभ गयी, खूंटे-सी गड़ गयी। वह खूंटा और अधिक पुख्ता हुआ फिल्म में हमारे सात वर्ष के कैरियर में। लेकिन जो सबसे
बड़ी चीज फिल्म ने दी हमको वह रोचकता बांटने की कला थी हम यह सोचते हैं कि जैसा
हमारे बीच चलता था, किशोर कभी कहते
कि पंडित, सिगरेट नहीं
पियेगा ?" (तब तो स्टूडियो
में सिगरेट पी सकते थे, अतः सिगरेट पीने
का मौका दे दिया जाता 1) इस तरह बात चल
पड़ती थी तो यह जो रोचकता बांटने की कला थी वह यहां फिल्मी समाज में पुख्ता हुई।
लेकिन इसका साहित्यिक रूप बाद में निखारा समझ लीजिए लगभग ४४-४५ में हालांकि फिल्म
तब अभी छोड़ी नहीं थी, लेकिन फिल्म से
उचट गये थे। दूसरे यह लगने लगा कि जिसको तुम दुकानदारी का माल बना कर बेचते हो वह
खरा माल है, उसको दूसरी
दृष्टि से देखो। वस्तुतः हुआ यह कि पहले तो एक धक्का लगा, बम्बई में जहाज फटा था
बड़ा भारी विस्फोट हुआ उसका उससे एक झटका लगा मन को। दूसरा बंगाल का अकाल-
अज्ञेय -
वह तो फिर '४२-४३ की बात
होगी ?
नागर हाँ, ४३ में हम गये थे कलकत्ता। फिल्म के ही काम से गये थे। कलकत्ता के चौरंगी में एक रेस्तरां में हम तीन-चार
आदमी बैठे हुए थे खाने के लिए। बाहर से एक. आदमो शीशे की दीवार से खूनी आंखों से
देखा रहा था।... तो यह रोचकता की बात है तो शुरू की कहानी की, लेकिन बाद में उसका पकड़ाव या उसका औपन्यासिक रूप, उसका संजोना, यह बाद की चीज है
अज्ञेय : लेकिन मैंने जो आपके पहले उपन्यास और बड़े
उपन्यास पढ़े- 'अमृत और विष', 'बूंद और समुद्र' तो वे रोचक तो बहुत से
(जिसे मैं गुण ही मानता हूं, आज भी गुण मानता हूँ) लेकिन उनमें मुझे यह भी लगा कि
कहीं-कहीं किसी को रोचक बनाने के लिए आपने ज्यादा विस्तार दिया है जो कि अनावश्यक
भी है, बल्कि वैसा न
होता तो कहानी ज्यादा जोरदार ही होती। आपको अब पीछे देखते हुए ऐसा लगता है, या आप ऐसा नहीं मानते ?
नागर - आप जब यह बात सुझाते हैं, स्वीकार करूं कि मुझे ऐसे
मौके याद आते हैं। कि मुझे भी लगा कि मैं कहीं अपने उस सिद्धान्त से, कि रोचक होना चाहिए, कहीं जरूरत से ज्यादा बंध
गया हूँ। आपकी बात के सुझाव से एकाएक हमारे मन में यह बात आती है। इसे स्वीकार
करता हूँ और मुझे आशा है कि आगे कुछ लिखूँगा तो शायद यह कमी हट जाएगी। लेकिन यह बात
सही है। अभी तक किसी ने मुझसे यह कहीं नहीं। मन में कहीं पर छिपा चोर था, लेकिन वह उजागर नहीं हुआ था।
अज्ञेय : कई एक प्रसंग ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत
आकर्षक है, लेकिन पूरा
उपन्यास देखने के बाद लगता है कि वे उसको आगे तो नहीं ले जाते।... अच्छा, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूं। आपके सब उपन्यासों में मुझको लगता रहा है कि
भाषा के प्रति आपके कान बहुत सजग हैं और भाषा का आपके लिए एक स्वतंत्र आकर्षण भी
है। एक तो यह दृष्टि है कि भाषा एक माध्यम है, आप कथा कह रहे हैं और उसके लिए भी भाषा आवश्यक है। लेकिन
भाषा की तरह-तरह की ध्वनियां है. उसके काकु हैं: उन सबको सुनना, उनको पकड़ना भी आपको
अच्छा लगता है, सिर्फ भाषा के
माध्यम के अंग के नाते नहीं, अपने-आप में आकर्षक आपके बहुत से चरित्र तरह-तरह की बोलियां
बोलते हैं। क्या ऐसा होता है कि आपका किसी बोली के या लहजे के या ढंग के प्रति
आकर्षण है या कि चरित्र जहां का है, जिस समाज का या जिस युग का है, उसका निर्वाह करने के लिए
आप उसके अनुरूप भाषा का प्रयोग करते हैं।
नागर नहीं, बोली के आकर्षण से नहीं करता हूँ, चरित्र को देख कर करता
हूं। यह हो सकता है कि चरित्र गढ़ने में कि मानसिक नक्शे में हमने एक चरित्र समाज
से लिया, तो उसको ठीक वैसे
नहीं रखता; उसके साथी-संघाती
जो होते हैं तीन-चार ऐसे समान-धर्मा कैरेक्टर, उनमें से चुन कर और जोड़ कर एक कैरेक्टर बनता है। ये तीन
चार पात्र जो इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे उनमें से किसी के बात करने का ढंग आकर्षित करता है तो
वह ले लिया, एडॉप्ट कर लिया और
बाद में उसको कुछ और प्रोढ़ा लिया। 'बूंद और समुद्र में' ताई थी, दो-तीन, कैरेक्टरों में से ताई बन गयी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि
बोली- बानी पहले आ गयी हो,
फिर चरित्र आया
हो।
अज्ञेय : जैसे आगरा की बोली है। आपने तो उसमें पूरा एक
उपन्यास लिख डाला-सेठ बांकेमल। तो उसके मूल में क्या प्रेरणा थी ?
नागर उसमें जो सेठ बांकेमल है वह असल में सेठ सुर्रोमल
हैं और हमारे चौबेजी हमारे छोटे मामा। उनका बात करने का ढंग - बोली तो स्वाभाविक
रूप से आकर्षित करती है, लेकिन उनका बात
करने का ढंग, जिस लच्छेदार ढंग
से वे बात करते थे, वह भी बड़ा
प्यारा लगा। पूरा एक जमाना ले गये वे लोग फिर आ गया दूसरा जमाना।
अज्ञेय : इनके वास्तविक चरित्र ऐसे आकर्षक थे ?
नागर हाँ, उन्हें वैसे का वैसा ढालने का प्रयत्न किया। एक और मजे की
बात सुनाऊं। पुस्तक छपने के लिए सोचा उनका फोटोग्राफ ले लें। सेठजी से कहा कि आप
फोटोग्राफ खिंचवायें। सवेरे ही वह फतुही, दुपल्ली टोपी और धोती पहने हुए आ गये। बगल में अंगरखा, पगड़ी, दुपट्टा ले कर आये और फोटोग्राफर
के यहां चलने लगे, 'भैया, तू भी ठीक है— मैंने सोची
तू ठीक कहवे है, मर जाऊंगो तो
लौंडे कहेंगे 'हाय बाबू हाय
बाबू' तो कहूंगो, 'जे टंगे हैं तेरे बाबू'।' यानी इस टाइप के
आदमी थे, छूते थे मन को।
अज्ञेय : अच्छा, अगर आपको याद हो तो आप क्रम से, जिस क्रम से लिखे गये या
प्रकाशित हुए, अपने उपन्यासों
के नाम बता दीजिए ?
नागर: एक जो अप्रकाशित है, अभी तक रखा है कहीं फाइल
में, वह '३७-३८ का है कामरेड
प्रेमदास। पूरे 'देवदास' की पैरोडी की थी चकल्लस
में, क्योंकि वह फिल्म
ऐसी छा गयी थी। पूरी पैरोडी की थी। कामरेड प्रेमदास उसका नाम था। दूसरा उपन्यास
अधूरा रहा, खुदा का घर। अभी
भी उसके चार-पांच अंक पड़े होंगे। यह शायद '३९ का लिखा हुआ है। तीसरा '४१ में लिखा बांकेमल। यह आगरा की बोली में है।
चौथा भूख के नाम से बाद में प्रकाशित हुआ। फिर बूंद और समुद्र, फिर अमृत और विष। अमृत और
विष के आस-पास अवध के चक्कर लगाये और गदर के फूल लिखा, गांव-गांव से किस्से बटोर कर। उसके बाद शतरंज
के मोहरे उपन्यास। फिर वेश्याओं के इंटरव्यूज हैं ये कोठेवालियां। सुहाग के नूपुर
दक्षिण भारत की कोवलन कन्नगी की कथा पर उपन्यास है। लेकिन यह उपन्यास मैंने मांग
पर लिखा, ईमान से आपसे
कहता हूं। एक बार दिल्ली में डॉ. सावित्री सिन्हा एक मीटिंग में हमसे झगड़ पड़ी
थीं कि आप इसको बुरा क्यों कहते हैं ? बुरे की बात नहीं है. इतना ही कि वह मैंने अपने मन से प्रेरित
हो कर नहीं लिखा था। कथा थी पास में पड़ी हुई। इस पर रेडियो नाटक भी लिख चुका था; सत्यकाम विद्यालंकर ने
धर्मयुग में मांगा मैंने वह लिख दिया बहाने से सुहाग के नूपुर। फिर हम आ गये एकदा
नैमिषारण्ये में एकदा नैमिषारण्ये के बाद मानस का हंस। उसके बाद खाली वक्त में
चैतन्य महाप्रभु लिख दिया जीवनी के रूप
में। फिर नाच्यौ बहुत गोपाल, फिर खंजन नैन। कहानी-वहानी, नाटक-फाटक बीच-बीच में चलते रहे।
अज्ञेय : आपके पहले के जो शुरू के उपन्यास थे उनमें
ज्यादातर अपने समकालीन समाज के चित्र थे, वहीं से आप रोचक चित्र उठाते थे और उसकी एक बड़ी आकर्षक
कहानी होती थी। उनके बाद फिर सुहाग का नूपुर में पहली बार, चाहे किसी भी कारण
सेफरमाइश पर ही सही आप दूसरे युग की कथा में गये। लेकिन बाद के उपन्यासों में
नाच्यो बहुत गोपाल को छोड़ कर अधिकतर आप किसी पहले के ऐतिहासिक युग में गये हैं।
क्या यह तब से स्थायी परिवर्तन हुआ-
नागर स्थायी परिवर्तन तो नहीं कह सकते। मन की दोनों
ही धाराएं थीं। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक धारा की शुरुआत कोवलन कत्रगी की
कहानी के बहाने से शुरू हुई। लेकिन जब उदयशंकर की फिल्म लिखने गया था कल्पना और
सुब्बलक्ष्मी की मीरा का डबिंग किया तो छः महीने रहा था वहां पर वहीं पर हमको बूंद
और समुद्र के लिए नाम कम-से-कम वहां मिला, प्रेरणा मिली। उसके नोट्स, शुरू के नोट्स वहीं बनाये थे। एकदा नैमिषारण्ये
भी मन में वहीं उतरा। कपालेश्वर का बहुत बड़ा मंदिर था। वहां पन्द्रह-बीस सुनने
वालों को ले कर बैठता था हाँ पन्द्रह-बीस सुनने वाला को ले कर बैठता था कथा-वाचक।
तो देखा, कथा-वाचक की बोली अलग हो जाती है उसके लहजे-लटके तो
करीब-करीब वही जो हमारे उत्तर भारत में हैं। फिर मन में हुआ कि 'नैमिषारण्ये' को कथा ही क्यों
कही जाये - अयोध्या है, और बड़े-बड़े शहर हैं, गोमती के किनारे
नैमिषारण्ये ही क्यों ? मन में यह कीड़ा लग गया। धीरे-धीरे उसके बहाने
बढ़ता रहा, पढ़ता भी रहा। डोनाल्ड मैकेंजी के मिथ्स एंड लेजेंड्स के भी
करीब-करीब सभी वोल्यूम्स देख गया-चाट गया। इस तरह एक रुचि तो उधर चली गयी और बनी
रही।
उसी समय एक बात और भी हुई थी। देश का पहले-पहला बिखराव आ
रहा था भाषाओं को ले कर भाषा वाले प्रदेशों को ले कर तभी झगड़े शुरू हुए थे।
जवाहरलाल के जमाने में। काशीप्रसाद जायसवाल से एक सूत्र मिला कि कुशाणों को निकाल
देने बाद वाकाटकों के समय में एक महान सांस्कृतिक आंदोलन हुआ होगा। तो हमारा
नैमिषारण्ये तो भरों का इलाका था। इसलिए वहां से वह मिला। तो गंगा, सिंधु, सरस्वती सारी
नदियों के जल से पश्लिक नल के नीचे बाल्टी लगा कर नहा रहा था, और यों सारी
नदियां नहा रहा था ! वहाँ से एक यह आइडिया स्ट्राइक हुआ। तुलसीदास तो घुट्टी में
मिले ही थे। सीधी बात थी इसी को ले कर महेश (कौल) को छेड़ते रहते थे, फिर हमने सोचा, इसी को ले कर हम
उपन्यास लिख डालें तो उसमें लिख दिया।खंजन नैन वस्तुतः लिखना नहीं चाहता था, ऐसी कोई अकुलाहट
मन में नहीं थी। पर इधर-उधर बाहर से पाठकों के काफी पत्र आये। फिर चतुःशती आने को
थी। विश्वनाथजी (राजपाल एंड सेज के) भी कहने लगे, 'पंडितजी, आप हमको पहले यह
लिख दीजिये।" चारों तरफ से खींच-तान होने लगी ... हमारी दादी थीं, अंधी हो गयी थीं।
बचपन का पहला शॉक, पहला धक्का लगा दादी का अंधा होना। वह कहीं मन
को छूता था। संयोग की बात कि जब हम हो ना की स्थिति में थे तब दादी को सपने में
देखा तो और भी मन को लगा। वस्तुतः सूरदास हमारे मन के नायक नहीं है। तुलसी में तो
कुछ पौरुष था। सूरदास तो बेचारे पर फिर उनके कुछ पदों में लगा कि वह भी इतना
संघर्ष झेल कर आये है। फिर पदों से एक और सूत्र हमको मिल गया कि सूरदास वाराणसी भी
गये थे। सूरदास के आस-पास बहुत-सी प्रांतियां फैल गयी थीं, फैली हुई थीं।
उनसे थोड़ी-सी चिढ़ हुई। इन सब बातों की वजह से खंजन नैन लिख लिया।
अज्ञेय : पढ़ने वालों में बहुत-से लोगों को मानस का हंस
ज्यादा अच्छा लगा 1 आप क्या सोचते हैं कि सूर और तुलसी के ही चरित्र में जो अन्तर
था उसके कारण आपकी भी रुचि सूर में कम थी; या कि सूर के जो देवता है, कृष्ण और तुलसी
के हैं राम, उनमें भी अंतर है और उसके कारण भी उपन्यासकार को सुविधा या
असुविधा होती है ?
नागर: आपने बड़ी पकड़ की बात कही। श्रद्धा तो एक ही
जगह से उमगती है, चाहे राम और चाहे कृष्ण को ले कर। लेकिन जो
मुझे मिले वह राम मिले। यानी मैं तो शिव का उपासक शिव भक्ति तो संस्कारवश घर से ही
नाता था, लेकिन मुझे जो मिले वह राम मिले। वह थे एक राम वाला बाबा तो
राम का बोध जाग गया मन में। इस प्रकार से सीता-राम मेरे इष्ट हैं, इसमें कोई शक की
बात नहीं। आपको एक और मजे की बात बताऊं। खंजन नैन लिखते समय श्याम तो राम बन जाते
थे। मगर सीता राधा नहीं बनती थी। लिखते मन उचट जाता। एक तरफ ध्यान न लगता तो फिर
उसके बाद वह धारा बहती नहीं थी, सुर नहीं बैठते थे। फिर ऐसे में हमको याद। आया
कि गोपीनाथ कविराज की एक पुस्तक थी श्रीकृष्ण प्रसंग, वह हमने पढ़ी थी—
ध्यान आया कि उसमें राधा के संबंध में कुछ विवरण था। अमा कला को उन्होंने डिफाइन
किया है। फिर हम को दिक्कत नहीं रही। राधा को हम लोग जो परकीया स्वकीया के भेद से देखते
हैं, लिखते हैं, वह सब हम लोगों के दिमाग में आलरेडी भरा है।
फिर अमा कला में, सीता में कोई अंतर नहीं आया। यह बात जरूर
बतलाऊंगा। बाकी राम को श्याम बनाने में हमको दिक्कत नहीं हुई।
अज्ञेय : नागरजी, एक बात और आपसे पूछना
चाहता हूँ। आपके उपन्यासों में देखता हूं कि वैष्णव मंदिरों का संदर्भ जरूर रहता
है और पुजारियों के ऐसे-ऐसे चित्र आप प्रस्तुत करते हैं जो बड़ा सूक्ष्म
पर्यवेक्षण मांगते हैं। इसका आधार क्या है ? आपका उन परिवारों से
संबंध रहा या कि...
नागर : दादी के साथ गोकुलद्वारा और दूसरे मंदिरों
में बहुत घूमा। बचपन में कुछ परिवारों से भी संबंध रहा। मुहल्ले में रहिये तो सब
रंग मिल जाते हैं। उसका भी एक प्रभाव कह सकते हैं। इस तरह भी बहुत मिला।
अज्ञेय : नहीं, नागरजी, सिर्फ मुहल्ले
में रहने की बात तो नहीं, उससे कुछ ज्यादा है। क्योंकि मंदिर के भीतर के
संगठन की बारीक जानकारी भी उपन्यासों में है।
नागर : यह तो स्वाभाविक रूप से है। जैसे कि
गोकुलद्वारे का है। वहां कीर्तनियों वगैरह की पुष्टि मार्ग की परंपरा चली आयी है।
मुझे यह नहीं मालूम था कि यह पुष्टिमार्ग की पद्धति है, लेकिन यह
शिवा-मंगला ... यह सब करते-करते और फिर और भी कैरेक्टर्स हैं, मुहल्ले में पास
ही रहते हैं, बहुत दूर नहीं-उनकी बातचीत कानों में पड़ती रहती।... हां, शुरू में, भाई, एक गुण ने मुझे
उपन्यास लिखने की प्रेरणा दी। आपने जैसा संकेत किया, मेरे कान सचमुच बड़े सजग
हैं। बातें सुनने में बहुत तेज हैं और दूसरे साथ-ही-साथ इधर-उधर भाव-भंगिमा देखने
में आनंद आता है। सोचता हूं कि इस तरह यदि मैं लेखक न बनता तो एक्टर अच्छा बनता, डायरेक्टर अच्छा
बनता।
अज्ञेय : यह तो है-उपन्यासों में बहत ही बारीकी से
देखी हुई चीजें भी आती हैं। और बहुत ध्यान से सुनी हुई भी। इससे ज्यादा कोई निजी
आकर्षण मंदिर के ही वातावरण का भी रहा ? या पूजा-अर्चना में निजी
प्रवृत्ति रही या कि वैसा कुछ नहीं है ?
नागर मन में एक आस्तिक संस्कार तो घर के वातावरण से
था ही। जैसे तुलसीदास घुट्टी में मिले -घंटा-भर रोज पढ़ते थे और अभ्यास डालने के
लिए नित्यप्रति सुनते थे। तो तुलसीदास तो घुट्टी में मिले। श्लोक भी बहुत याद थे।
गंगालहरी मुझे कंठस्थ थी। तो यह संस्कार मिलते रहे। घर में ही बहुत अधिक सात्विक
संस्कार था। शुरू में यह था कि जनेऊ के बाद बाहर का खाना हमारे लिए बंद हो गया।
था। यो एक संस्कार तो आप कह सकते हैं कि हमको घर से मिला। एक बात मैं अपने लेखक
होने के साथ भी जोड़ सकता हूँ। वह आस्था बाद में जिंदगी की मार खा कर बम्बई में
मिली। '४३ में बाबा रामजी मिले। साधारण आदमी लेकिन गजब का आदमी।
उसकी वजह से बदला, मन में भी बदलाव आया। वह कहें, पागलों का
पाखाना-पेशाब उठाओ, उनको खराब की हुई दरियां धुलवाओ न करें तो 'बाबू' बनें उनकी नजरों
में बुरा। वह टोक, 'रामजी राम, आंखों में आंखें डाल के
देखो रामजी झांकत हैं कि नहीं!' उनकी लड़त ने मुझे छुआ। ये जो चीजें थीं, मन को छू गयीं, उनके प्रति
दृष्टिकोण बदला। जैसा आपसे शुरू में कहा, फिल्म में रहते हुए
रोचकता जरूर बढ़ी क्योंकि वहां वह बहुत जरूरी थी, लेकिन इन सारी चीजों में
जो दुकानदारी का तत्व था, वह जीवन के सिद्धांत के रूप में गहराई में बाबा
रामजी से समझ में आया।
अज्ञेय : अब दूसरी तरह के प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं
जो लेखक से लेखक पूछता है। यह बताइये कि जो उपन्यास आपने लिखे-खास कर इधर के
जिनमें ऐतिहासिक वस्तु थी— उनमें एक ऐतिहासिक युग को ले कर या उस दूसरे युग की प्रतीति
कराने के संदर्भ में कुछ खास तरह की समस्याएं आपके सामने आर्थी -जैसे युगीन संवेदन
की समस्या ?
नागर : भाई, जैसे तुलसीदास मान लीजिये।
तुलसीदास नायक की तरह से-मन में एक जगह हैं—उनके सम्बन्ध में रचनाएं भी काफी पहले
से पढ़ी थीं। जब हम तुलसीदास को नायक बना कर सोचने लगे तो यह हुआ कि उनका ऐतिहासिक
रूप गलत न हो इसलिए सजावट के लिए हमने उसे इस्तेमाल किया। सूरदास के सम्बन्ध में
अपने मन की कच्चाई भी बता दूं-पकड़ भी है, दोनों ही बातें हैं-
-सूरदास हमने इतना ही पढ़ा था, जितना स्कूल में कोर्स में पढ़ाया गया। बाद में
उनके पदों के दो-चार छोटे-मोटे संग्रह पढ़ लिये थे। पूरा सूरसागर कभी पढ़ने का
मौका नहीं मिला था। जैसे रामचरितमानस पहले से पढ़ा था,, कवितावली पढ़ी थी, उस तरह
सूर-साहित्य का बहुत निकट का परिचय मुझे नहीं था। जब सूर के ऊपर मन लिखने के लिए
बाहर से, भीतर से प्रेरित हो गया तो इस रूप से ऐतिहासिक बैकग्राउंड
जानना मेरे लिए अनिवार्य हो गया। सूर का ठीक-ठीक वही समय है जब कि सूफ़ी और सन्त
हमारे इस टूटे हुए मन को समाज उत्थान लेते हैं, उसको उबार लेते हैं जैसे
वाराह ने पृथ्वी को उबार लिया था तो वह सब पढ़ना जरूरी था। इसमें एक बार रचना से
पहले सारा इतिहास पढ़ा, उसके नोट बनाये। लेकिन अभी वह जमाना ही जमाना
खाली दिमाग में कूद रहा है। दूसरी तरफ सूरसागर भी पढ़ा था - साथ-साथ पढ़ते थे।
उससे सूर के चित्र मन में आने लगे, कैसे वर्णन कर रहे हैं, कैसे वह कहते हैं
मैं जूझेंगा, टरूंगा नहीं। इससे उनके मन के विभिन्न मूड कुछ खुलते। वह
देखते हुए जब दोनों को, इतिहास को और निजी चरित्र को साथ में लेता हूं
तब कहानी कहीं बनने लगती है।....तो इसमें यह जरूर हुआ कि पहले इतिहास को मुझे जम
कर पढ़ना पड़ा, नहीं तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था। इसी बहाने से बहुत पढ़ा, पढ़ता गया। मेरा
काम हुआ कि मेरा काम नहीं हुआ उससे मतलब नहीं; लेकिन उस बहाने पढ़ाई खूब
हुई। सत्रह-अठारह बरस तक उस सब्जेक्ट के पीछे रहे। लिखा बहुत बाद में दोनों बातें
होती है। 1 इस तरह से पहले एक कैरेक्टर के लिए और बाद में सजावट के लिए या उसके
देश-काल की आवश्यकता का अनुभव करते हुए भी आ जाती है। एक बात और भी आप देखेंगे, भाई, कि चाहे इतिहास
में गया है चाहे आज के जमाने में रहा हूँ, व्यक्ति और समाज का नाता
मैंने किसी भी हालत में छोड़ा नहीं है। चाहे एकदा नैमिषारण्ये में रहा हूँ तो भी
समाज को चित्रित करते हुए उसमें व्यक्ति को देखा है, चाहे तुलसी बाबा या सूर
बाबा के इतिहास में रहा हूँ वहाँ भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा।
अज्ञेय अब दूसरी तरह के प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं
जो लेखक से लेखक पूछता है। यह बताइये कि जो उपन्यास आपने लिखे- खासकर इधर के
जिनमें ऐतिहासिक वस्तु थी उनमें एक ऐतिहासिक युग को ले कर या उस दूसरे युग की
प्रतीति कराने के संदर्भ में कुछ खास तरह की समस्याएं आपके सामने आयी जैसे युगीन
संवेदन की समस्या ?
नागर भाई, जैसे तुलसीदास मान
तुलसीदास की तरह से मन में एक जगह है उनके संबंध में रचनाएं भी काफी पहले से पढ़ी
थीं। जब हम दासको नायक बना कर सोचने लगे तो यह हुआ कि उनका ऐतिहासिक रूप गलत न हो
इसलिए सजावट के लिए हमने उसे इस्तेमाल किया। सूरदास के संबंध में अपने मन को
कच्चाई भी बता हूँ- पकड़ भी है, दोनों ही जाते हैं सूरदास हमने इतना ही पढ़ा था।
जितना स्कूल में कोर्स में पढ़ाया गया। बाद में उनके पदों के दो-चार छोटे-मोटे
संग्रह पढ़ लिए थे। पूरा सूरसागर कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला था। जैसे
रामचरितमानस पहले से पढ़ा था. कवितावली पड़ी थी, उस तरह सूर साहित्य का
बहुत निकट का परिचय मुझे नहीं था। जब सूर के ऊपर मन लिखने के लिए बाहर से, भीतर से प्रेरित
हो गया तो इस रूप से ऐतिहासिक बैंक जानना मेरे लिए अनिवार्य हो गया। सूर का
ठीक-ठीक यही समय है। जबकि सूफी और संत हमारे इस टूटे हुए मन को समाज उत्थान लेते
हैं, उसको उतार लेते हैं जैसे वाराह ने पृथ्वी को उबार लिया था
तो वह सब पढ़ना जरूरी था। इसमें एक बार रचना से पहले सारा इतिहास पड़ा उसे नोट
बनाए। लेकिन अभी वह जमाना ही जमान खाली दिमाग में कूद रहा है। दूसरी तरफ सूरसागर
भी पड़ा था- साथ-साथ पढ़ते थे। उसके सूर के चित्र मन में आने लगे, कैसे वर्णन कर
रहे हैं, कैसे वह कहते हैं कि मैं जुगा रूंगा नहीं। इससे उनके मन के
विभिन्न मूड कुछ खुलते। वह देखते हुए जब दोनों को, इतिहास को और निजी चरित्र
को साथ में लेता हूँ तब कहानी कहीं बनने लगती है। ...तो.. इसमें यह जरूर हुआ कि
पहले इतिहास को मुझे जम कर पढ़ना पड़ा, नहीं तो रास्ता ही नहीं
मिल रहा था। इसी बहाने से बहुत पढ़ा, पढ़ता गया। मेरा काम हुआ
कि मेरा काम नहीं हुआ। उससे मतलब नहीं; लेकिन उस बहाने पढ़ाई खूब
हुई। सत्रह- अठारह बरस तक उस सब्जेक्ट के पीछे रहे। लिखा बहुत बाद में। दोनों
बातें होती हैं। इस तरह से पहले एक कैरेक्टर के लिए और बाद में सजावट के लिए या
उसके देश-काल को आवश्यकता का अनुभव करते हुए भी आ जाती है। एक बात और भी आप
देखेंगे, भाई, कि चाहे इतिहास में गया हूं चाहे आज के जमाने
में रहा हूँ, व्यक्ति और समाज का नाता मैंने किसी भी हालत में नहीं छोड़ा
है। चाहे एकदा नैमिषारण्ये में रहा हूँ तो भी समाज को चित्रित करते हुए उसमें
व्यक्ति को देखा है, चाहे तुलसी बाबा या सूर बाबा के इतिहास में रहा
हूँ वो भी
व्यक्ति को नहीं छोड़ा।
अज्ञेय : आपने इतने उपन्यास लिखे है आपको आज सबसे अधिक
संतोषजनक कौन-सा मालूम होता है ?
नागर भाई, अभी जवाब नहीं दूंगा। अभी
मन में एक-आध और है।
अज्ञेय : वह तो रहना चाहिए। असल बात यह है जो जो आगे
लिखेंगे वही सबसे अच्छा है। पर मैं अपनी बात को उलट कर यो भी पूछ सकता है कि कोई
ऐसा उपन्यास है जिसके बारे में आप सोचते हैं। कि इसे आज लिखता तो दूसरी तरह लिखता ?
नागर हो है. एकदा नैमिषारण्ये। इसके लिए सचमुच मन
में होता है कि एक बार अगर इसको फिर से लिख यो शायद अच्छा लिखे। यो पिछले जो भी
हैं उनमें कुछ थोड़ा-सा परिवर्तन तो हर जगह करने का जी चाहेगा। लेकिन जैसे बूंद और
समुद्र है, उसका मैं चाहूंगा जैसा है वैसा ही रहे. अमृत और विष जैसा है
वैसा हो रहे। लेकिन एकदा नैमिषारण्ये के लिए मन में जरूर होता है कि इसको मैं एक
बार फिर से लिख जाऊं हालांकि कह नहीं सकता कि उसका मौका मिलेगा।
अज्ञेय : लेकिन क्यों-किस दृष्टि से ? नागर इस दृष्टि
से कि हमको यह अनुभव हुआ कि जो पौराणिक कथाएं हमको छुट्टी में मिली थी- मुहल्ले
में कथा वार्ता बहुत सी होती थीं— उनके पास, या उनसे, जो रंग मिले, उनके पास हमारा
जो नया पाठक है- यानी जिसने तुलसी को पढ़ कर भी मुझे पत्र लिखे वह पाठक, मेरा नया पाठक
उसके पास नहीं आ पाता। वह एकदा नैमिषारण्ये के पास भी नहीं आ पाया। उसका कारण क्या
है ? हम जो बात सहज ढंग से पौराणिक बेस बना कर लिख गए, कह गए, हमारे मन में तो
उस तरह से है। पर उस बेचारे के पास वह बेस नहीं है। यह बड़ा खटकता है। कहीं-कहीं
पर उसको पढ़ कर पाठक छायावादी हो जाता है। यह हमको बहुत अच्छा नहीं लगता। यानी ऐसा
लगता है कि मेरा जो उद्देश्य था वह....
अज्ञेय अगर यह बात आपका अनुमान सही है कि पाठक के पास
वह आधार नहीं है तो उसका आप क्या इलाज कर सकते हैं ?
नागर उन कहानियों को थोड़ा रोचक ढंग से इलैबोरेट
करूं। जिस बात पर आपने टोकाउस बात का इस्तेमाल जरूर करूंगा ताकि थोड़ा और अधिक
रोचक ढंग से कहानियां पातक पहुँच जाएं, यानी उनका बेस ले कर वे
मेरी बात आगे देखें।
अज्ञेय : लेकिन उसका मतलब क्या यह नहीं हो जाएगा कि आप
उपन्यास में कथा रखने के अलावा पाठक को कुछ जानकारी देने का भी काम कर रहे हैं- जो
वास्तव में उपन्यासकार का उद्देश्य नहीं है।
नागर उद्देश्य नहीं है, यह सही बात है।
मैं मानता हूँ। लेकिन कभी-कभी सोचता हूँ कि ये कहानियां क्यों नहीं पहुंचती पाठक
तक। अज्ञेय : जैसे आजकल बहुत से लोग लिखते हैं और उनके मन में कहीं यह खयाल रहता
है इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, इसका विदेशी पाठक होगा तो वे कुछ टूरिस्टी
किस्म की टूरिस्ट के उपयोग की जानकारी उसमें दे दें ! नागर हां हां नहीं उस तरह का
मन नहीं है।
अज्ञेय : तो फिर कैसे हल करेंगे इस समस्या को ?
नागर अब यहाँ हल है कि उन कहानियों दो ऐसे कहा जाए
कि पाठक के मन को पकड़ से। जैसे मान लीजिए, 'हरिहर' है। उसका उदाहरण
लूं। हरि-हर को कथा, जिसने शैव: और वैष्णव को जोड़ा जिसकी लड़ाइयों
में किम और वैष्णव को जोड़ते है- उसमें कथा बना ली कि नारद ने बहुत तप किया अपने
मानस-पिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए वह प्रसन्न हुए, उनसे वरदान मांगा
कि जिसको चाहूँ मैं लड़ा दूं। ब्रह्मा को मजबूरन वर देना पड़ा। उसके बाद नारद ने
हरि की हर से शिकायते को और कुछ शिकायतें हर को हरि से कों, और दोनों को
लड़वा दिया। यह तो पुराण कथा है। अब नारद को मैं द्वंद्व का प्रतीक मानता है, जो मन के द्वंद
को उजागर कर देता है। इस बात को जरा और सफाई से लिख जाऊ तो शायद वह जो पकड़ है-
उपदेश देने की बात नहीं है उस चीज को लिखने की सफाई अगर और आ जाए तो शायद मैं नए
पाठक के मन को किसी हद तक पकड़ लूंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ।
अज्ञेय : यह जो आपने नए पाठक के साथ लेखक के संवाद की
समस्या बताई, इसके लोगों ने कई तरह के उत्तर दिए हैं। उदाहरण के लिए, यशपाल ने अगर 'दिया' लिखी, या राहुलजी ने
दूसरे युग की घटना ले कर कुछ उपन्यास लिखे, उनके सामने यह समस्या उस
रूप में नहीं आनी क्योंकि विशेष रूप से राहुलजी ने (जो कि विद्वान थे उन्होंने) उस
समय से सामग्री तो प्रामाणिक ली। वह सामग्री तथ्य या घटना की दृष्टि से तो प्रामाणिक
है, लेकिन संवेदन और मनोविज्ञान की दृष्टि से गलत हो जाती है।
उन्होंने सब चरित्रों को आधुनिक बना दिया। इससे एक तरफ तो आज के पाठक को सहायता
मिलती है, वह उन भावनाओं को पहचानता है। लेकिन उस युग में उस स्थिति
से वह भावनाएं नहीं होती थी, इस दृष्टि से वे चरित्र झूठे हो जाते हैं। एक
दूसरी तरह की चीज हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखन में थी। वह तो इस मामले में सजग
थे कि जानकारी भी देनी है- मुझसे उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं ऐसे उपन्यास लिखना
चाहता हूँ जिनमें मैं पाठकों को जानकारी भी दूँ, और यह काम उन्होंने किया
भी। उनके उपन्यासों में दूसरे युग के जो चित्र आते हैं वे इस दृष्टि से झूठ नहीं
होते। उनमें वहिरूप भी जो है वह भी उस युग का है और जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त की
हैं वे भी युगानुरूप हैं, उन्हें आधुनिक नहीं बनाती। चीजों को ऐसे जोड़ा
जरूर है, ऐसी चीजें अवश्य ली है जो....
नागर जो मन को भी छू जाती हैं।
अज्ञेय हो। तो दोनों में आपको कौन-सा रास्ता.... नागर
आपने जो दूसरी बात कह दी वही मेरे पास भी है। कुछ भावनाएं ऐसी होती है हर काल में
एक प्रकार का मनोच नहीं घूमता फिर भी बहुत-सी बातें ऐसी होती है, जो आज भी हमको
छूती है, चार हजार वर्ष पहले भी छूती थीं। मान लीजिए शकुंतला को
विदाई और कण्व का दुखी होना। आज भी घर मैं ऐसे क्षण आ जाते हैं। उनको ले कर अगर हम
आगे बढ़ जाते हैं, उनकी थोड़ी-सी छाया जरूर स्पर्श करते हैं। कहीं
आप उस काल की मनोभावनाओं तक भी जाएंगे क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम खाली
मनोभावनाओं को ही छू कर चले जाएं। यह दिकत भी है। तो हम छुएंगे जरूर, लेकिन उस छूने के
साथ-साथ हम आगे भी बढ़ेंगे, उस काल की मनोभावनाओं को चित्रित करने का
लक्ष्य रखेंगे। अगर हम खाली छू कर रह जाएंगे तो यह लक्ष्य अधूरा रह जाएगा।
अज्ञेष नागरजी, मैंने जो नाम लिए-
राहुलजी और द्विवेदी का यह दोनों तो पहले पंडित थे और बाद में उपन्यासकार। आप तो
पहले किस्सागो हैं (मेरी बात गलत न समझे !) उनकी समस्याएं तो काफी अलग-अलग रहीं।
आप फिर कुछ और विस्तार से बताएंगे कि आप क्या सोचते है, ऐसी स्थिति में
क्या करना ठीक होगा पाठक से संवाद बनाए रखने के लिए और वस्तु के प्रति सच्चे बने
रहने के लिए ?
नागर: देखिए, लिखते समय तो हम न पाठक
देखते हैं, न अपना मन देखते हैं। उस समय तो मन बहता है। जो चरित्र हमने
अपने मन में पचा लिया, जो स्थिति या विचारपद्धति पचा ली, वह चलता है।
वैसी बहुत-सी समस्याएं आती हैं। पांडित्य से लगाव है, उसको छुए बिना हम
कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते, पात्र को आगे नहीं बढ़ा सकते। पर भाई, जब तक वह हमको पच
नहीं जाएगा, हम नहीं लिखेंगे।
डॉ. मनोज रस्तोगी के सौजन्य से