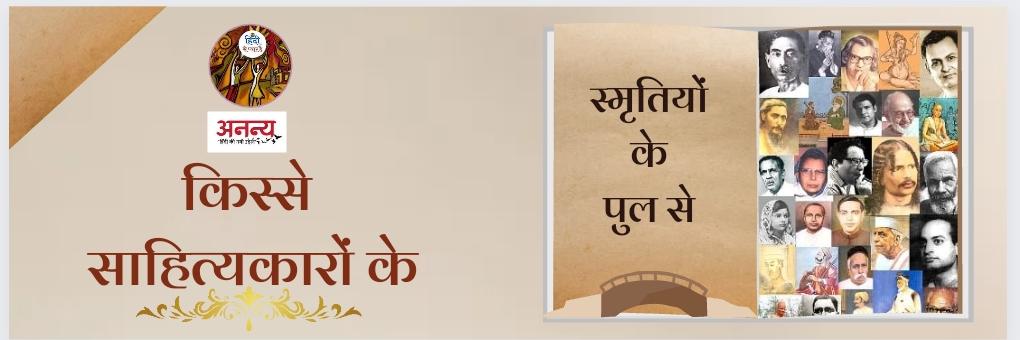डॉ० नगेंद्र को आज याद करना, पूर्णतः श्वेत हो चुके केशों के साथ श्याम केश युग में विचरण करने सा है। यह ऐसा है जैसे कोई शांत स्थिर तालाब में कंकड़ी-सा गिर जाए और उसमें पड़ते गोलाकार स्मृति व्यूह के साथ अतीत तल की गहराई तक पहुंच जाएं आप ही सोचें कहां आभासित दुनिया के संग मोबाईल होने को विवश करता 2019 के सजे-धजे बाजार का वातानुकूलित भीड़तंत्र और कहां 1969 की गलियों मोहल्लों में धेला पैसा इक्कनी, दुक्कनी आदि वाली मिट्टी में लोटी-पोटी, छाबछी वाले से झुंगा मांगती दिल्ली। लालटेन से कंप्यूटर युग तक आए. मुझ जैसा जीव जब अतीत में झांकता है तो आह! ग्राम्य जीवन भी क्या था की तर्ज पर गाता है।
डॉ० नगेंद्र मेरी स्मृतियों में अनेक रूपों में जीवित है हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा - साहित्य के अप्रतिम विद्वान, दबंग प्रशासक दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को अपने परिवार की तरह विकसित करते मुखिया हिंदी आलोचना को नया मुहावरा देता प्रखर आलोचक आदि न जाने और क्या - क्या ! इस और क्या में विरोध के अनेक झंझावत झेलता, अपनों से हारकर अंततः पराजित योद्धा - सा अकेलेपन को भोगता महारथी भी है। पद पर बैठा जब लाल बुझक्कड़ देवता समान पूजा जा सकता है तो पद पर बैठा विद्वान तो स्वतः पूजनीय हो जाता है। पद पर बैठा व्यक्ति तो शहद का छत्ता होता जिसके हर कोण से मधु ग्रहण करने को ज्ञानीजन पदासीन का इतना मधुमय महिमामंडन करते हैं कि अंततः उसे मधुमेह हो जाता है और और वह अशक्त हो जाता है। आप तो जानते हैं कि आज के युग में ही नहीं अनंत काल से आवश्यक्तानुसार अपने देवता गढ़ने और उनकी पूजा अर्चना द्वारा अपना मनोवंछित पाने की अटूट पंरपरा है जीव आवश्यक्तानुसार देवियों देवों देवों के देवों आदि का शरणागत होता रहा है। धन की आवश्यक्ता हुई तो लक्ष्मी मैया के चरण गह लिए, संकट आया तो संकटमोचन हनुमान के नाम पर मंगलवार को प्रसाद बांटने लगे देवी और देवता के नाम में ही दे वर्ण है अतः वर्णानुसार वे भक्त को देते रहते हैं। पद पर बैठा आदमी भी देवी या देवता होता है।
पदासीन डॉ० नगेंद्र भी अनेक के लिए देवादिदेव रहे हैं मेरे लिए एक गुरु रहे जिनसे मैंने कामायनी राम की शक्ति पूजा, अरस्तू का काव्यशास्त्र, उर्वशी जैसी कालजयी रचनाओं के गर्म और साहित्यिक सौंदर्य को जाना। उनके गुणवत्तापूर्ण अध्यापकीय पक्ष के चाहे समर्थक हों. विरोधी हों या 'गुटपिरपेक्ष आदि अनादि सभी प्रशंसक रहे हैं जिन्होंने उनसे पढ़ा वे तो प्रशंसक हैं हीं पर जो नहीं पढ़ पाए वे विवशता में अपने हाथ मलते हुए प्रशंसा करते हैं। डॉ० नगेंद्र से पढ़ने के सुख का वर्णन गूंगे के गुड़ जैसा है। मुझे आज भी 1970-71 के वे दिन याद हैं जब हम ढाई बजे होने वाली डॉ० नगेंद्र की क्लास की कमरा नंबर 65 में या 18 में प्रतीक्षा करते थे। कक्षा का समय 3.20 तक का था और हमारी यूनिवर्सिटी स्पेशल बस 330 पर जाती थी। 90 प्रतिशत की यू स्पेशल छूटती ही थी पढ़ाते समय न तो डॉ० नगेंद्र को समय का ध्यान रहता था और न ही पढ़ने वाले को समय पर कक्षा छूट जाए तो यू स्पेशल मिल जाती और में 20 किलोमीटर दूर अपने निवास रामकृष्ण पुरम् साढ़े चार बजे के लगभग पहुंच जाता अन्यथा उस समय की गरीब परिवहन व्यवस्था की कृपा से शाम के सात तो बज ही जाते । पर कोई शिकायत नहीं।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने न केवल मुझे आजीविका दी अपितु रचनात्मक साहित्य का विस्तृत आकाश भी दिया। इस विश्वविद्यालय ने मुझे एक ऐसा परिवार दिया जिसमें निरंतर वृद्धि हुई। मेरा जन्म 1949 में इलाहबाद में हुआ था और उस समय साहित्य की राजनीति और राजनीति की राजनीति की कर्मभूमि इलाहबाद ही थी। इलाहबाद में पैदा होने और निराला की गली से गुजरने के बावजूद साहित्य का कीड़ा मेरे बचपन को प्रभावित नहीं कर पाया। पिताजी का जब दिल्ली तबादला हुआ तो मैं मात्र नी वर्ष का था।
इसके बाद की मेरी शिक्षा-दीक्षा की उत्तरदायी दिल्ली है। निचले स्तर की स्कूली शिक्षा से लेकर 'उच्च स्तर की शिक्षा मैंने दिल्ली के आंगन में खेलते-कूदते ग्रहण की है।
मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और मैंने बी ए में मैथ्स आनर्स लिया था पर एक कहानी ने मुझे 1966 में हिंदी आनर्स का छात्र बना दिया और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हस्तिनापुर कालेज से हिंदी आनर्स करने लगा। मैं आभारी हूं इस कॉलेज का कि इसने मुझे शून्य से ज्ञान की बूंद बनाने में भूमिका निभाई। इसी कॉलेज में पढ़ी नीव के कारण मैने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में 40 वर्ष पढ़ाया, चार वर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में अतिथि आचार्य के रूप में पढ़ाया। एक व्यंग्य लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई लेखन के लिए अनेक सम्मानों से सम्मानित एवं पुरस्कृत हुआ। इसी कालेज ने मुझे नरेंद्र कोहली और कैलाश वाजपेयी जैसे गुरु दिए। सतगुरु मिल जाए तो शिष्य का जीवन सुधर जाता है, उसे सही मार्ग मिल जाता है अन्यथा सत शिष्यों के कंधे पर चढ़े गुरु से गोविंद बने अपना जीवन सुधारते हैं और उन्हें विलासिता का सच्चा मार्ग मिल जाता है। नरेंद्र कोहली मेरे लिए सतगुरु हैं जो न तो स्वयं अंधत्व धरण करते हैं और न ही शिष्य को अंधत्व धारण करने की राह में धकेलते हैं। लेखन उनके जीवन की प्राथमिकता है जिसके लिए वे किसी भी प्रकार का मोह त्याग सकते हैं। इस प्राथमिकता के चलते ही उन्होंने सन् 2008 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की लगी लगाई एसोसिएट प्रोफेसर की सुविधाजनक नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। डॉ० नगेंद्र ने उनकी पत्नी मधुरीमा कोहली से सकोध कहा- नरेन्द्र का दिमाग खराब हो गया है। पढ़ाते हुए भी लेखन किया जा सकता है। मैंने किया है उसे कहो, त्यागपत्र वापिस ले।" पर इस अर्थ में नरेन्द्र कोहली जिद्दी है। लेखन के बिन अन्य सब कुछ सून है। लेखन उनके लिए तपस्या और साधना है और वे सहन नहीं कर सकते कि इसमें कोई राक्षस वृत्ति बाधा पहुंचाए।
आरंभ में मैंनें प्रेम प्रकाश निर्मल प्रेम प्रकाश शैल तथा परीक्षित कुंद्रा के नाम से कहानियां और कविताएं लिखीं । उन दिनों कैलाश वाजपेयी के प्रभाव में मैंनें आधुनिक कविताएं लिखीं तो पाठयक्रम में जयशंकर प्रसाद की लहर ने मेरे रोमानी होते युवा मन को छायावाद दिया। इस कारण छायावदी प्रभाव की कविताएं भी लिखीं। पर धीरे-धीरे नरेन्द्र कोहली के प्रभाव में कविताएं छोड़ भी दीं। इन गुरुओं की साहित्यिक अभिरुचि एवं प्रभाव के कारण ही हमारे कालेज में उस समय के अनेक महत्वपूर्ण साहित्यकार आए। डॉ० नरेन्द्र कोहली के प्रयासों से हरिवंश राय बच्चन हमारे कॉलेज में आए थे। इस अवसर पर उन्होंने अपनी रचनाएं बड़े मन से सुनाई फूलमाला ले लो लाई है मालन बड़ी दूर से गीत हो या फिर उस समय चर्चित मधुशाला के सस्वर पाठ ने सभी को उनका दीवाना-सा कर दिया। कविता प्रतियोगिता में प्रथम आने का पुरस्कार मैंने बच्चन जी से ग्रहण किया। यह डॉ० नरेन्द्र कोहली का ही प्रभाव था कि कॉलेज के वार्षिकोत्सव पर कोई राजनेता मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाया गया, अपितु रामाधरी सिंह दिनकर को इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया। 'दिनकर' ने अपनी कुछ कविताएं एवं गीत सुनाए। उस समय हमारे पाठ्यक्रम में कुरुक्षेत्र था, छात्रों को आग्रह पर उन्होंने इस खंडकाव्य के कुछ अंश सुनाए तथा परशुराम की प्रतीक्षा के भी कुछ अंश ।
सन् 1965 से सन् 1975 के समय को यदि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का स्वर्णिम समय कहूं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी । इसे डॉ० नगेंद्र का पराभव काल भी कहूं ता भी अत्युक्ति न होगी। उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग तथा उससे संबंद्ध विभिन्न महाविद्यालयों के हिंदी विभाग में डॉ नगेंद्र विजयेंद्र स्नातक निर्मला जैन सावित्री सिन्हा मन्नु भंडारी, रामदरश मिश्र, नित्यानंद तिवारी, इंद्रनाथ चौधुरी अजित कुमार महीप सिंह नरेंद्र मोहन, नरेंद्र कोहली इंदु जैन सुरेश सिन्हा कैलाश वाजपेयी विश्वनाथ त्रिपाठी गंगा प्रसाद विमल डॉ० हरदयाल, विनय, स्नेहमयी चौधरी पुष्पा राही, विनय आदि जैसे साहित्यिक व्यक्तित्व थे। उस समय हिंदी विभाग की धरती बहुत उर्वर थी । उर्वर अब भी है पर कुछ और वस्तुओं के लिए उस समय हिंदी विभाग में युवा रचनाकारों की एक बड़ी साहित्यिक सेना थी। उन दिनों ही दिविक समीकरण जैसे सहयोगी संकलन निकले थे। यही नही तत्कालीन विभागाध्यक्षा सावित्री सिन्हा के प्रधान संपादकत्व एवं डॉ रामदरश मिश्र, सुरेश ऋतुपर्ण, रमेश शर्मा, मधु जैन के संपादक मंडल ने 1971 मुट्ठियों में बंद आकार निकला था। इसमें मेरी भी कहानी थी – डरपोक।
उस समय हिंदी आलोचना में दो ध्रुव थे डॉ० नगेंद्र और डॉ० नामवर सिंह कहा जाता है कि डॉ० नामवर सिंह को डॉ० नगेंद्र ने यथाशक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय में घुसने न दिया पर धीरे-धीरे दिल्ली विश्वविद्यालय में उनके अनेक प्रशसंक पैठ बना रहे थे। इसी कारण 1969 के आसपास डॉ० नगेंद्र के खिलाफ अनेक क्रांतिकारियों ने आंदोलन आरंभ किया परिणाम सुखद निकला, डॉ० नगेंद्र विभागाध्यक्ष से पद से मुक्त हुए परिणाम इतना सुखद निकला कि अनेक कातिकारियों को नौकरियां मिल गई।
इधर डॉ० निर्मला जैन की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आई है दिल्ली शहर दर शहर इस कृति में उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली के अनेक चेहरों को साक्षात किया है। इस कृति में उन्होंने अपने समय के हिंदी विभाग के अनेक चेहरों को भी प्रत्यक्ष किया है। डॉ नगेंद्र को उन्होंने बहुत समीप से देखा और परखा है। हमारे समय में वे हम जैसे युवाओं की चहेती प्रध्यापिका थीं वे विश्वविद्यालय में अपनी जमीन तैयार करने को प्रयत्नशील हर युवा साहित्यकार की साथी थीं। उन्होंने डॉ० नगेंद्र के व्यक्तित्व का सटीक चित्रण किया है। निश्चित ही जितना डॉ० नगेंद्र को उनके सहयोगी जानते थे उतना जानने की हमारी औकात ही कहां है उनकी संगति से तो हम परिचित हो सकते थे पर उनकी विसंगति की परख तो डॉ० निर्मला जैन जैसा नजदीकी जानकार ही कर सकता है। वे लिखती हैं, डॉ. नगेन्द्र के व्यक्तित्व में जो गरिमामय आतंक दिखाई पड़ता था. वह उन्होंने बड़े जतन से अर्जित करके ओढ़ लिया था। धीरे-धीरे ये उसी को अपना स्वभाव मानने लगे। भीतर से वे शायद उतने मजबूत और सुरक्षित नहीं थे। यह बात उनके निकट के लोगों को वर्षों बाद समझ में आई। वे स्वयं अपने व्यक्तित्व की व्याख्या नारियल की उपमा देकर किया करते थे पर दिक्कत यह थी कि ऊपर का कवच टूटने न पाए. इसके बारे में वे बड़ी सावधानी बरतते रहे। रूप-रंग और सलीकेदार वेशभूषा से वे सामनेवाले को जितना सम्मोहित करते थे स्वभाव की कठोरता और रौबीली औपचारिकता से उतना ही दूर फेंकते थे। जिस दिन वे कक्षा लेते हुए हँस देते थे. विद्यार्थियों के लिए वह दुर्लभ अनुभव का क्षण होता था। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति कर्तृर्तव्य निष्ठा और कर्मठता थी और सीमा हठाग्रह और लचीलेपन का लगभग अभाव। जीवन हो या साहित्य, औरों के लिए गुंजाइश देने या अपनी गलती को स्वीकार करने में उन्हें अपनी हेठी लगती थी किसी प्रसंग में अगर वह मन ही मन दूसरे को सही मान भी लेते थे, तो घुमा-फिराकर बात को ऐसा मोड़ देते थे कि अन्ततः पक्ष उनका ही सही उनकी इस बनावट में उनकी सामन्ती विरासत और आर्यसमाजी संस्कारों का मिला-जुला योगदान था। विचित्र बात यह थी कि सत्ता के गलियारों में उनकी विनम्रता देखते बनती थी पर उनमें सत्य निष्ठा और औचित्य-बोध कम नहीं था. जिसके बल पर उन्होंने एक बार भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश को बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिया था। उनके साहस के ऐसे अनेक उदाहरण है।"
एम. ए. में प्रसाद स्पेशल लेने के कारण जयशंकर प्रसाद मेरे प्रिय साहित्यकार बन रहे थे। कामायनी से अधिक मैं उनके नाटको से प्रभावित था और यहीं मुझमें व्यंग्य के प्रति रुचि भी जग रही थी। इसी रुचि के कारण मैंने अपने एम ए के लघुशोध प्रबंध का विषय प्रसाद के नाटकों में हास्य-व्यंग्य ' मांगा। यह विषय समिति के अध्यक्ष डॉ० नगेंद्र के लिए झटका सा था। कामायनी जैसे महाकाव्य के रचयिता गुरु गंभीर प्रसाद के साहित्य में हास्य व्यंग्य ! विषय मना कर दिया गया। डॉ० नगेंद्र बहस का अवकाश नहीं देते थे वैसे तो मुझपर दबाव डाला जा रहा था कि मैं रीतिकाल स्पेशल लूं और उसी पर लघु शोध प्रबंध लिखूं क्योंकि मेरे हितचिंतक प्राध्यापक को विश्वास था कि इस कारण मेरी प्रथम श्रेणी अवश्य आएगी पर नरेंद्र कोहली के प्रभाव में मैं आधुनिक साहित्य में रुचि ओर लेखकीय महत्त्वाकांक्षा के कारण पथ भ्रष्ट हो चुका था अतः इसस पथ भ्रष्ट जिद्दी को प्रेम चंद की कहानियों में सामाजिक परिवेश दिया गया। ये दीगर बात है कि एम फिल के लिए लघु शोध प्रबंध का विषय मुझे यही मिला। क्योंकि तब तक डॉ० नगेंद्र विश्वविद्यालय में आई कांति का शिकार हो चुके थे और विभागाध्यक्ष पद पर डा विजयेंद्र स्नातक, जो आधुनिक युग के प्रति उदार थे, आसीन हो चुके थे।
डॉ नगेंद्र को किसी विद्यार्थी ने हंसते नहीं देखा था। इस बात का जिक निर्मला जैन ने अपनी कृति में किया है। हम विद्यार्थियों के बीच उनका आतंक ऐसा था कि हंसने वालों की हंसी रुक जाती थी। 1970 में एम फाईनल के विद्यार्थियों को शुभकामना और विदाई देने के लिए आर्टस फेक्लटी में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मैंनेएक नाटक में अभिनय भी किया था। मेरे लिए एक और अविस्मरणीय विजेता वाला क्षण वह रहा जब मैंने डॉ० नगेंद्र को हंसा दिया। लोगों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से हंसते देखा। इस कार्यक्रम में मैंने अपनी एक व्यंग्य रचना काम पीड़ित आलोचक पढ़ी। यह प्रसाद की 'कामायनी की पैरोडी थी। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने किसी महाकाव्य की कथा की पैरोडी की है। उसका एक अंश देता हूं- एक बर्फ का कारखाना था, जहां काम कम और आराम अधिक होता था, क्योंकि सर्दियों के दिन थे एक दिन अचानक वहां के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि दूसरे कारखाने का मालिक यह चाहता था। मज़दूरों के नेता ने अपनी मांग रखी कि उन्हें विलास के वह समस्त साधन उपलब्ध होने चाहिए जो कारखाने के मालिक को हैं। इसके साथ ही गुप्त रूप से उसने यह सलाह भी दी थी कि यदि मालिक, केवल मजदूरों के नेता को ही समस्त साधन व्यक्तिगत रूप में दे दे, तो हड़ताल नहीं होगी। (छायावाद में व्यक्तिवादी स्वर) मजदूरों का मालिक नहीं माना और और मजदूरों ने क्रान्ति आरम्भ कर दी हड़ताल हुई। पुलिस आई गोलियां चलीं और एक मजदूर को छोड़कर सारे मजदूर मारे गए। कारखाना उजड़ गया। उस बचे हुए मजदूर का नाम मनु था वह अति वीर और शक्तिशाली था।
एक अन्य नगर में एक और बर्फ का कारखाना था जिसके मालिक का नाम काम था। उसने मनु को देखा और उसे अपना मैनेजर बनाने का निश्चय किया। मनु को आकर्षिक करने के लिए उसने अपनी श्रद्धा नाम की पुत्री को भेजा श्रद्धा नीली साड़ी पहनकर मनु के सामने आयी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बिजली के सफेद बल्ब पर नीला कागज चढ़ा दिया गया हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों मन ही मन शरमाए और शरमाकर एक दूसरे से प्रेम करने लगे (छायावाद में प्रेम और सौन्दर्य) इस प्रेम से श्रद्धा गर्भवती हुई और काम को विश्वास हो गया कि अब मनु अवश्य उनके हाथ में आ जाएगा।
'इड़ा' नाम की एक नारी इड़ावृत्त देश की प्रधानमंत्री थी। वह मनु को वहां का राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, क्योंकि वह एक मजदूर था ( छायावाद में साम्यवाद का संकेत) उसने अपने दो प्रतिनिधियों (चमचों) को मनु को लाने के लिए भेजा। उन प्रतिनिधियों के नाम आकृति और किलात थे। उन्होंने मनु को विलास के रंग में डुबोना आरम्भ किया और मनु डूब गए। इसके पश्चात् उन्होंने हड़ा का संकेत उनसे कहा। मनु ने कहा, तुम लोग चलो में आता हूँ।
मनु श्रद्धा को रात के समय उसी प्रकार छोड़कर चले गए जिस प्रकार अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए थे। काम को जब यह पता लगा तो उसने मनु को फटकारा और मुकदमा करने की धमकी दी। मनु पहले घबराए फिर सोचा अब तो वह राष्ट्रपति बन जाएंगे अतः अन्तिम विजय उनकी निश्चित है' आदि आदि।
मैं डॉ निर्मला जैन के इस निष्कर्ष से सहमत हूं – 1956 से 1968 तक डॉ. नगेन्द्र ने दिल्ली की साहित्यिक गतिविधियों में व्यक्ति की नहीं, संस्था की भूमिका निभाई। विश्वविद्यालय में तो उनका दबदबा था ही प्रशासन में उप-कुलपति के पद के अलावा शायद ही कोई पद ऐसा रहा हो जिस पर उनकी नियुक्ति न हुई हो। दूसरे विभागाध्यक्षों के ऊपर वे बराबर भारी पड़ते थे। उनकी राय की हर उपकुलपति ने कद्र की। उन्होंने बड़ी सूझ-बूझ और निष्ठा से पाठ्यक्रम बनाए। विभाग में अनुसन्धान परिषद् का गठन किया। शिक्षा मन्त्रालय की सहायता से हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय कायम किया। वर्षों दिल्ली विश्वविद्यालय का हिन्दी विभाग पूरे देश के लिए मॉडल बना रहा। कॉलेजों की बढ़ती संख्या के कारण उन्होंने सैकड़ों नियुक्तियों की जिनमें उनका मुख्य सरोकार विषय और कॉलेज का हित रहता था। जाति-धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से ये धुन-चुनकर योग्य व्यक्तियों को विभाग और स्थानीय कॉलेजों में लाते रहे।"
अपने समय में डॉ नगेंद्र ने स्वगीय सुख का आनंद लिया तो अपने पराभव काल में लगभग नारकीय कष्ट को भी भोगा। डॉ० नगेंद्र के जीवन के उपेक्षित समय का भी मैं साक्षी रहा हूं। वैशाली, पीतमपुरा दिल्ली में रहने वाले पड़ोसी और साहित्यकार जानते हैं कि अपने अंतिम समय में वे कितने असहाय थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो बहुत असम्मानजनक वातावरण था। उनके अपने ही उनसे छिटके दिख रहे थे।
प्रसाद के लहर संग्रह में एक कविता है- मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी इसी में वे कहते हैं-छोटे-से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ? मुझे भी लगता है कि मेरे जीवन में, कुछ वर्ष के छोटे से जीवन में आए. डॉ नगेंद्र की बड़ी कथाएं कब तक और कितनी कहूं क्या अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता अब मीन रहूं मैं? मेरे कानों में तो निरंतर डॉ० नगेंद्र की धीर गंभीर बुलंद आवाज में, दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्टस फेक्लटी के कोनों को गुंजायमान करती, राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां गूंज रही है, जिसे क्षमा याचना सहित मैं कुछ परिवर्तन से प्रस्तुत कर रहा हूँ- रवि हुआ अस्त
ज्योति के पत्र पर लिखा
अमर रह गया अपराजेय समर
असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार
…………………………………………………………………………………………………………….
डॉ० प्रेम जनमेजय की स्मृति से
……………………………………………………………………………………………………………
| व्हाट्सएप शेयर |