मोहन राकेश एक अप्रतिम साहित्यकार थे जिन्हें 'नई कहानी' आंदोलन का प्रणेता भी कहा जाता है और 'आधुनिक नाटक का मसीहा' भी। मेरा सौभाग्य कि मुझे उनका साथ और सहयोग मिला। उनके नाटकों का में प्रथम शोधार्थी था। दिल्ली विश्वविद्यालय से एम. लिट्. की उपाधि हेतु मुझे उनके नाटकों पर शोध का विषय आसानी से नहीं मिला। बात 1970 की है, एम.ए. के परीक्षाफल के आधार पर प्रथम तीस विद्यार्थियों को दो वर्षीय एम. लिट्. में प्रवेश प्राप्त होता था। इन तीस में से उस वर्ष में भी एक था। विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोध विषय आबंटन हेतु चयन समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता 31. नगेन्द्र कर रहे थे। सदस्यों में डॉ. विजयेन्द्र स्नातक, डॉ० सावित्री सिन्हा, डॉ. दशरथ ओझा और डॉ. उदयभानु सिंह भी थे। ये सभी हिंदी के जाने-माने विद्वान् थे और एम.ए. में हमारे शिक्षक भी।
मेरा क्रम आया, मेैं तनिक घबराहट के साथ भीतर गया, डॉ० नगेन्द्र ने मुझसे पूछा कि मैं किस विधा पर विषय चाहता हूँ। मैंने उत्तर दिया, 'नाटक पर'। डॉ० नगेन्द्र ने। पूछा कि क्या मैंने कोई विषय सोचा है। जैसे ही मैंने उत्तर दिया, 'मोहन राकेश के नाटकों का विवेचन', वे भड़क उठे, 'मोहन राकेश के नाटक? नहीं नहीं इस पर नहीं हो सकता। प्रसाद पर ले लो भारतेंदु पर ले लो। मोहन राकेश पर क्यों लेना चाहते हो वो तो अभी नए हैं!" मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, 'श्रीमन्! वे आज के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं उनके नाटकों ने हमारी पीढ़ी को बहुत प्रभावित किया है।"
डॉ. नगेन्द्र को मेरा उत्तर उपयुक्त नहीं लगा। उनके सामने विद्यार्थी तो क्या अध्यापक भी अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर पाते थे। नगेन्द्र जी ने कहा, 'मोहन राकेश ने अभी लिखे ही कितने नाटक हैं?" मेरे मुख से फूट पड़ा, जी जितने कालिदास ने।' डॉ. नगेन्द्र को इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। सावित्री सिन्हा जी ने स्थिति को अनुकूल बनाते हुए बड़े प्रेम से कहा, हरीश, डॉ. साहब ठीक कह रहे हैं तुम भारतेंदु या प्रसाद पर विषय ले लो" मैंने निवेदन किया, श्रीमन मोहन राकेश के नाटक उनसे आगे की सोच के नाटक हैं, मुझे उन पर ही विषय दे दीजिए। डॉ. सावित्री सिन्हा ने नगेन्द्र जी की ओर देखा। नगेन्द्र जी बोले, 'देखो, मोहन राकेश अभी युवा लेखक हैं और वैसे भी हम प्रायः जीवित साहित्यकारों पर शोध नहीं करवाते।'
उनका कथन मुझे तीर सा चुभा, मैं खड़ा हो गया और यह कहकर कि, 'मैं फिर उनपर उनके बाद ही शोध करूंगा', कक्ष से बाहर निकल गया। मैं रुआंसा हो गया था और कला संकाय के उत्तरी कॉरीडोर में जाकर मुंडेर पर बैठ गया। चिंतन करने लगा कि मैंने ठीक किया या ग़लत। मुझे लगने लगा कि मैंने ग़लत ही किया, प्राध्यापक पद पाने के लिए एम. लिट्. करना आवश्यक है भले ही शोध का विषय कोई भी हो। मैं यह सोच-सोच भी दुखी होने लगा कि डॉ. नगेन्द्र जैसे सम्मानित और समर्थ विद्वान् गुरु की अवहेलना मैंने कर दी है, इससे मेरा करियर प्रभावित हो सकता है। मुझे पछतावा होने लगा था कि मुझे ऐसा करके अशालीन नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने सपने टूटते नज़र आने लगा मुझे लगा कि अब बात बिगड़ गई है, ठीक न हो सकेगी क्योंकि मैंने अभद्रता की। मुझे वॉकआउट नहीं करना चाहिए था....
मैं अभी चिंता निमग्न ही था कि वहाँ हिंदी विभाग का सेवा कर्मचारी ईश्वर चंद आया और मुझसे बोला, 'तुम्हें नगेन्द्र जी बुला रहे हैं।' उसका आना उस समय मुझे सच में सर्वशक्तिमान ईश्वर का आना ही लगा। मैं उसके साथ चल पड़ा और निश्चय कर लिया कि. जो भी जैसा भी विषय मिलेगा वह स्वीकार कर लूंगा।
मैं सिर झुकाए कक्ष में प्रवेश कर गया और डॉ. नगेन्द्र जी की वाणी मेरे कानों में गूंजी, ‘यह कोई तरीका है, चलो जो विषय बोलोगे समिति दे देगी।' इस प्रकार मुझे सौभाग्य मिला कि में मोहन राकेश पर शोध करने वाला प्रथम शोधार्थी बन सका।
मोहन राकेश जी तक यह बात पहुँच गई। मैं जब अपने शोध के सिलसिले में उनसे मिला तब उन्होंने बताया कि उन्हें डॉ. दशरथ ओझा जी ने पूरी घटना बताई थी। इस घटना के कारण भी वे मुझे अपने करीब पाते थे। शोध के सिलसिले में अब मेरा उनसे मिलना अक्सर होने लगा। मैं उनके नाटकों से संबंधित जिज्ञासाओं का ढेर उनके पास लेकर जाता और वे जब उनका शमन करने लगते थे तो प्रायः एक-आध सवालों का जवाब देने में एक- दो घंटे निकल जाते। वे उन पात्रों में खो जाते जिनकी नाट्य सृष्टि उन्होंने ही की थी। वे मल्लिका के बारे में, सावित्री के विषय और सुंदरी के बारे में बताते-बताते भावुक हो जाते।। भावावेश में कही गई उनकी बातों का बहुत सारा प्रतिशत मेरे पल्ले तक नहीं पड़ता था। एक शाम तो हद हो गई. हम रिवोली सिनेमा हॉल की रेस्तरां में बैठे थे। फिल्म चल रही थी।
इसलिए रेस्तरां में उस समय केवल हम दोनों ही वहाँ थे। मोहन राकेश जी कुछ बताते बताते कहीं खो गए और फिर अत्यंत भावुक होकर कहने लगे, 'मैं ही हूँ, महेन्द्रनाथ, बार-बार घिसा जाने वाला रबर का टुकड़ा में ही हूँ। नंद भी मैं ही हूँ मातुल भी में ही और कालिदास भी और जाने क्या हिंदी में बोलते-बोलते वे अँग्रेज़ी में बोलने लगे। मुझे यह लग रहा था कि वे रो न पड़े। इसके विपरीत जब वे पंजाबी में कभी कोई जालंधर या अमृतसर की घटना सुनाते अथवा मेरी कोई बात उन्हें विनोदप्रिय लगती, वे बहुत ज़ोर से खुलकर हँसते बल्कि ठहाका लगाते। उनका ठहाका दीवार की सफेदी का चूना गिरा सकता था।
मैं सोच-सोचकर बहुत खुश होता था कि मेरी कुछ बातें उनसे मिलती हैं। मेरा जन्म भी आठ जनवरी को हुआ, पंजाब में ही हुआ, मुझे भी अपनी माँ से अतिशय प्रेम था और मुझे भी दोस्तों के साथ महफिल जुटाने में बहुत आनंद आता है। मैंने सिवाय जन्मदिन के मिलान के बॉकी बातें उनसे साझा नहीं कीं। मोटे चश्मे के पीछे चमकती उनकी आँखें कुछ कह जाती थीं। बहुत उन दिनों उनका नाटक 'आधे-अधूरे' एक युग प्रवर्तक नाटक के रूप में हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच का सर्वाधिक चर्चित नाटक हो रहा था। मेरे नाट्य शिक्षकों में डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल जैसे प्रख्यात नाटककार भी थे जो मुझसे यदा-कदा उलाहने के स्वर में पूछ चुके थे कि मैं उनके नाटकों की तुलना में, जिनकी संख्या मोहन राकेश के नाटकों से अधिक है, राकेश के नाटकों को क्यों अधिक महत्त्व देता है। इस पर मैंने उन्हें जो बताया वह में राकेश जी को बताकर अच्छा समीक्षक होने का तमगा पा चुका था। मैंने अपनी सीमित बुद्धि से आकलन करते हुए पाया था कि डॉ. लाल यद्यपि अच्छा नाटक लिखते हैं और लिखने से पूर्व योजना बना लेते हैं कि किस शैली या शिल्प और किस प्रकार के मंच के लिए लिखना है। वे चरित्रों को अपने नियंत्रण में अनुशासित करते हैं। जबकि मोहन राकेश कोई बड़ी योजना नहीं बनाते चरित्र सृष्टि के विषय में सोचते हैं और वे चरित्रों को अपने बंधन में नहीं रखते, उनके नाटक उनके चरित्रों के अनुसार गतिवान होते हैं इसलिए वे चाहकर भी पुरुष चरित्रों को स्त्री चरित्रों से अधिक प्रभावी नहीं बना पाए।
- अच्छे समीक्षक का तमगा मिलने से मेरा उत्साहवर्धन हुआ था और में मोहन राकेश के साथ उनकी आली पकड़कर उनके चरित्रों को समझने की कोशिश करता रहा।
सितंबर 1971 में मेरा चयन दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में हुआ। तब मुझे एम. लिट्. करते हुए एक वर्ष हुआ था. प्रीवियस की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। मैंने राकेश जी को अपने लेक्चर नियुक्त होने की खबर दी। वे बहुत खुश हुए और मुझे पंजाबी में शाबाशी देते हुए कहने लगे, 'हमारा हरीश प्रोफेसर हो गया। अभी तो इसने सिर्फ़ 'मोहन' पढ़ा है जब 'राकेश' पढ़ लेगा तो पता नहीं क्या बनेगा?" उनका संकेत एम. लिट. फाइनल उत्तीर्ण करने का था। फाइनल में ही लघु शोध प्रबंध विभाग में जमा कराना था।
एक दिन मोहन राकेश जी का हमारे घर, शाहदरा में फोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं चाँदनी चौक जाऊँगा? उन्हें ज्ञात था कि मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ दरीबा चाँदनी चौक में, जहाँ हम पहले रहा करते थे, जाता हूँ। मैंने कहा, 'हाँ बताइये क्या करना है।' वे बोले, 'तुम्हें पार्टी देनी है, तुम प्रोफ़ेसर बन गए हो न!' मुझे थोड़ा संकोच हुआ मैंने कहा, "ऐसा क्या?" उन्होंने कहा, 'हाँ पार्टी देनी है उसके लिए चाँदनी चौक से दरीबा कलां के जलेबी और समोसे ले आना' मैंने कहा, 'अच्छा जी, कितनी ले लूँ? उन्होंने कहा, पार्टी है सोच-समझकर ले आना।"
मैंने दादा जी और बीजी को बताया कि आज मुझे मोहन राकेश जी पार्टी दे रहे हैं। दोनों खुश हुए। बीजी ने हिदायत दी कि ज़रा अच्छे कपड़े पहनकर जाना और जलेबी समोसे रखने के लिए थैला जरूर ले जाना। तब मेरे पास कोई वाहन नहीं था, शाहदरा से चाँदनी चौक तक फोर-सीटर चलते थे जिन्हें फटफटिया कहा जाता था में फटाफट तैयार होकर फोर-सीटर से दरीबा पहुँचा और पार्टी का सोचकर मैंने अनुमान लगाया कि दस- बारह व्यक्ति तो जरूर होंगे। मैंने उसी हिसाब से समोसे और जलेबियाँ खरीद लिये और वहाँ से एक थ्री व्हीलर (तब उसे स्कूटर कहते थे) लेकर राकेश जी के घर पहुँच गया।
राकेश जी के यहाँ उनके मित्र (संभवतः) राजिन्दर पाल बैठे हुए थे। सिगार चल रही थी। मैंने थैला रखा। राकेश जी के पैर छुए और कहा कि आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, अभी पार्टी में सब लोग आएंगे उशसे पहले ही अपना आशीर्वाद दे दीजिए। उन्होंने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, 'लोग' जितने आने थे वो तो आ चुके। तू थैले भर के ले आया हम हफ्ता भर खाएँगे!' और फिर उनके ठहाके गूंजने लगे। उस पार्टी में उस दिन हम तीनों ने गला भर-भरकर जलेबी और समोसे खाए और तीन बार गिलास भर-भरकर चाय पी। हाँ उस दिन मैं भी उनके साथ ठहाके लगा सका और उनसे खुल सका, जिसका लाभ मुझे तब तक वे रहे मिलता रहा।
मैं शोध हेतु जो लिखता था. दरियागंज में राधाकृष्ण प्रकाशन के ऑफिस में अक्सर मोहन राकेश जी को दिखाता था। मोहन राकेश और राधाकृष्ण प्रकाशन के स्वामी ओमप्रकाश जी की गहरी मित्रता थी। मेरे परिवार का भी संबंध ओमप्रकाश जी के परिवार से था। उनकी पत्नी को में बुआ जी संबोधित करता था। मैंने बुआजी के ही घर में मोहन राकेश जी को पहले-पहल देखा था तब में हिंदू कॉलेज का विद्यार्थी था। कभी-कभी मैं और मेरे भाई हरेन्द्र जी बुआ जी को मिलने जाते थे। उनके बेटे अरविन्द के साथ मेरे भाई हरेन्द्र जी की अच्छी जमती थी। अरविन्द भाई कालांतर में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट) के निदेशक भी रहे। राकेश जी ने ओमप्रकाश जी को मेरा लघु शोध-प्रबंध स्वीकृत होने के बाद उसे प्रकाशित करने को कहा था। वे मेरा लिखा पढ़ते नहीं, कहीं कहीं से सुनते थे और कहते थे कि यह डिग्री के लिए लिखा जा रहा है, जब प्रकाशित करना होगा, तब मैं पूरा पढ़ेगा और संपादन करूंगा। वे प्रोफेसरी कर चुके थे, उन्हें पूरा अंदाज़ा था कि शोध- प्रबंधों में कितना कुछ अनावश्यक लिखा जाता है जिसे वे 'पेज भराऊ' कहते थे। जब तक मेरा लघु शोध प्रबंध पूरा होता उससे पूर्व तीन जनवरी 1972 को सैंतालिस वर्ष की अल्पायु में मोहन राकेश का निधन हो गया।
वे नहीं रहे लेकिन उनका साहित्य, विशेष कर नाटक जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगी उनकी यादें, उनकी बातें, उनके ठहाके । 'शब्द' की सार्थकता पर कार्य करने वाले राकेश जी के शब्दों से सार्थक हुआ उनका साहित्य सदा जिंदा रहेगा।
हरीश नवल की स्मृति से
| व्हाट्सएप शेयर |
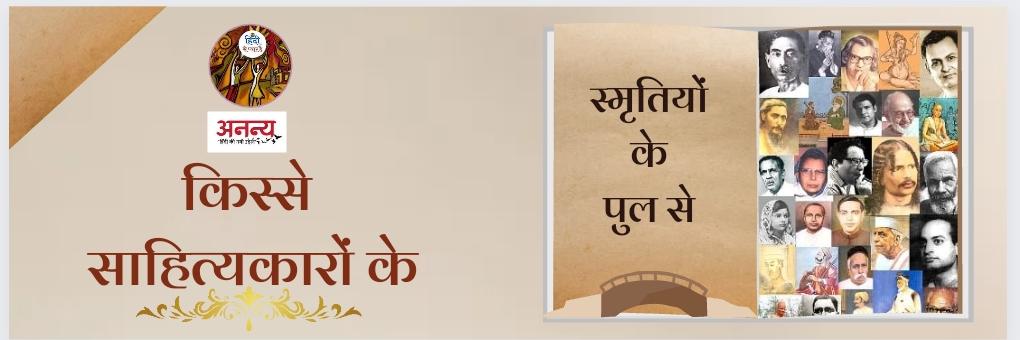
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें