निर्मल वर्मा से कुछ मुलाकातों का सौभाग्य मेरा भी रहा। उनसे पहली मुलाकात को आधार बना कर एक संस्मरण लिखा था। संस्मरणों की मेरी किताब 'दुनिया मेरे आगे' का वह पहला लेख है। आज उनके जन्मदिन पर फिर से साझा कर रहा हूं।
निर्मल स्मृति का वह एक चिथड़ा सुख
उन सीढ़ियों की अब बहुत धुंधली सी याद है।
स्मृति और कल्पना के मिले-जुले रसायन के बीच एक जीना उभरता है जिस पर अपने ही सहमे पांवों की पदचाप सुन रहा हूं।
ऊपर जाता हूं- यह भी याद नहीं है कि घंटी थी या सांकल।
लेकिन उस शख़्स का चेहरा साफ़-साफ़ याद है जिसने दरवाज़ा खोला था।
उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी- किसी आंतरिक शांति और करुणा के मेल से बनी हुई।
उसकी मृदु-कांपती आवाज़ ने पूछा था, किससे मिलना है।
मुझे उनसे नही मिलना था।
उनकी पत्नी से मिलना था।
यह सुनकर वे मुझे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गए।
हम दोनों पांच मिनट चुपचाप बैठे रहे।
न उन्होंने कुछ कहा, न मैंने।
उनकी पत्नी आईं तो वे चले गए।
यह 1994 का साल था।
वे निर्मल वर्मा थे- मेरे प्रिय लेखक।
लेकिन मैं उन दिनों पंकज बिष्ट के संपादन में निकलने वाली प्रकाशन विभाग की पत्रिका 'आजकल' के लिए गगन गिल का इंटरव्यू करने गया था।
जब निर्मल वर्मा सामने आ गए तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कहूं।
तो हमारे बीच चुप्पी बैठी रही।
.......
बरसों बाद गगन गिल ने मुझसे कहा कि तुम उस पहली मुलाकात का संस्मरण लिखो।
उन्हें याद था कि उस दिन ख़ूब बारिश हुई थी। उसी बारिश में वे मेरे लिए समोसे लेकर आई थीं।
मुझे और भी बहुत कुछ याद था।
वाकई उस दिन बहुत बारिश हुई थी- कई घंटे चली उस बारिश की वजह से मैं दो लोगों के उस परिवार में उस दिन फंसा रहा।
अजब हालत थी। बाहर के कमरे में मैं और गगन गिल क़रीब तीन घंटे बात करते रहे थे। इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था, उसके बाद की बातचीत भी। हम दोनों शायद एक-दूसरे से ऊब चुके थे। इस ऊब में यह बेचैनी भी शामिल थी कि एक तीसरा आदमी चुपचाप भीतर किसी कमरे में बैठा है। इस पूरी बातचीत के दौरान निर्मल बाहर नहीं आए थे।
तीन घंटों बाद जैसे पानी छूटा, हम दोनों ने राहत की सांस ली। मैं तत्काल उठा, मैंने नमस्ते करते हुए विदा ली।
लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने पूरी गली में घुटनों से ऊपर तक पानी जमा था। आगे बढ़ना मूर्खता थी, लेकिन वापस ऊपर जाना ऐसी अभद्रता होती जो मुझे मंज़ूर नहीं थी।
तो उसी पानी से मैंने गली पार करने का फ़ैसला किया। मैं धीरे-धीरे अपने पायंचे चढ़ा रहा था। लेकिन तभी अचानक सीढ़ियों से एक हड़बड़ाई सी मृदु आवाज़ आई- 'अरे, अरे। इस पानी में आप कैसे जाएंगे। ऊपर चलिए, ऊपर चलिए।'
मैंने मुड़़कर देखा, वही चमकती हुई करुण आंखें थी। निर्मल वर्मा हड़बड़ाए सीढ़ियां उतर रहे थे, जैसे मेरा हाथ थाम कर ले जाएंगे।
इसके बाद फिर मैं उसी ड्राइंग रूम में था। इस बार निर्मल जी के साथ भी। मैंने उन्हें बताया, मैं उनके लेखन का किस क़दर मुरीद हूं। 'एक चिथड़ा सुख' तब भी मेरा पसंदीदा उपन्यास था और अब भी है। बल्कि 1990 में जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो जैसे इस उपन्यास के किरदारों की उंगली पकड़ कर इस महानगर की सड़कें छानता रहा था। कनॉट प्लेस के प्लाजा के पास से निकलती, फिरोजशाह रोड के उन दिनों के सन्नाटे में एक पेड़ से लगकर रोती बिट्टी मुझे बार-बार याद आती। मॉल रोड पर विश्वविद्यालय के कैफे मे बैठे नित्ती भाई और इरा का खयाल आता। निजामुद्दीन की मस्जिद के पीछे की बसावट ध्यान खींचती। मंडी हाउस में कहीं होने वाले रिहर्सलों में चेखव और स्ट्रिनबर्ग के नाटकों का ज़िक्र याद आता। मेरे लिए यह गालिबो-मीर की नहीं, निर्मल वर्मा की दिल्ली थी- विश्वविद्यालय से मंडी हाउस और निजामुद्दीन से कनॉट प्लेस तक अपनी तलाश में भटकती हुई एक यात्रा की दिल्ली।
तो शाम की ओर बढ़ती हुई उस दोपहर को मैं इस दिल्ली के वास्तुशिल्पी के साथ- अपने प्रिय लेखक निर्मल वर्मा के साथ- बैठा हुआ था। वह एक यादगार शाम थी- हम तीनों, निर्मल वर्मा, गगन गिल और मैं देर तक बात करते रहे। मेरे लिए समोसे लाए गए जो मिल कर खाए गए। फिर सड़क का पानी घटा, मैं नीचे उतरा, और बारिश से भरे उस दिन में अपने भीतर लबालब भरा लौटा।
.......... निर्मल वर्मा जी को याद कर रहे हैं तो कुछ भाई प्रिय दर्शन जी की कलम से भी -
—
निर्मल वर्मा से कुछ मुलाकातों का सौभाग्य मेरा भी रहा। उनसे पहली मुलाकात को आधार बना कर एक संस्मरण लिखा था। संस्मरणों की मेरी किताब 'दुनिया मेरे आगे' का वह पहला लेख है। आज उनके जन्मदिन पर फिर से साझा कर रहा हूं।
निर्मल स्मृति का वह एक चिथड़ा सुख
उन सीढ़ियों की अब बहुत धुंधली सी याद है।
स्मृति और कल्पना के मिले-जुले रसायन के बीच एक जीना उभरता है जिस पर अपने ही सहमे पांवों की पदचाप सुन रहा हूं।
ऊपर जाता हूं- यह भी याद नहीं है कि घंटी थी या सांकल।
लेकिन उस शख़्स का चेहरा साफ़-साफ़ याद है जिसने दरवाज़ा खोला था।
उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी- किसी आंतरिक शांति और करुणा के मेल से बनी हुई।
उसकी मृदु-कांपती आवाज़ ने पूछा था, किससे मिलना है।
मुझे उनसे नही मिलना था।
उनकी पत्नी से मिलना था।
यह सुनकर वे मुझे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गए।
हम दोनों पांच मिनट चुपचाप बैठे रहे।
न उन्होंने कुछ कहा, न मैंने।
उनकी पत्नी आईं तो वे चले गए।
यह 1994 का साल था।
वे निर्मल वर्मा थे- मेरे प्रिय लेखक।
लेकिन मैं उन दिनों पंकज बिष्ट के संपादन में निकलने वाली प्रकाशन विभाग की पत्रिका 'आजकल' के लिए गगन गिल का इंटरव्यू करने गया था।
जब निर्मल वर्मा सामने आ गए तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कहूं।
तो हमारे बीच चुप्पी बैठी रही।
.......
बरसों बाद गगन गिल ने मुझसे कहा कि तुम उस पहली मुलाकात का संस्मरण लिखो।
उन्हें याद था कि उस दिन ख़ूब बारिश हुई थी। उसी बारिश में वे मेरे लिए समोसे लेकर आई थीं।
मुझे और भी बहुत कुछ याद था।
वाकई उस दिन बहुत बारिश हुई थी- कई घंटे चली उस बारिश की वजह से मैं दो लोगों के उस परिवार में उस दिन फंसा रहा।
अजब हालत थी। बाहर के कमरे में मैं और गगन गिल क़रीब तीन घंटे बात करते रहे थे। इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था, उसके बाद की बातचीत भी। हम दोनों शायद एक-दूसरे से ऊब चुके थे। इस ऊब में यह बेचैनी भी शामिल थी कि एक तीसरा आदमी चुपचाप भीतर किसी कमरे में बैठा है। इस पूरी बातचीत के दौरान निर्मल बाहर नहीं आए थे।
तीन घंटों बाद जैसे पानी छूटा, हम दोनों ने राहत की सांस ली। मैं तत्काल उठा, मैंने नमस्ते करते हुए विदा ली।
लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने पूरी गली में घुटनों से ऊपर तक पानी जमा था। आगे बढ़ना मूर्खता थी, लेकिन वापस ऊपर जाना ऐसी अभद्रता होती जो मुझे मंज़ूर नहीं थी।
तो उसी पानी से मैंने गली पार करने का फ़ैसला किया। मैं धीरे-धीरे अपने पायंचे चढ़ा रहा था। लेकिन तभी अचानक सीढ़ियों से एक हड़बड़ाई सी मृदु आवाज़ आई- 'अरे, अरे। इस पानी में आप कैसे जाएंगे। ऊपर चलिए, ऊपर चलिए।'
मैंने मुड़़कर देखा, वही चमकती हुई करुण आंखें थी। निर्मल वर्मा हड़बड़ाए सीढ़ियां उतर रहे थे, जैसे मेरा हाथ थाम कर ले जाएंगे।
इसके बाद फिर मैं उसी ड्राइंग रूम में था। इस बार निर्मल जी के साथ भी। मैंने उन्हें बताया, मैं उनके लेखन का किस क़दर मुरीद हूं। 'एक चिथड़ा सुख' तब भी मेरा पसंदीदा उपन्यास था और अब भी है। बल्कि 1990 में जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो जैसे इस उपन्यास के किरदारों की उंगली पकड़ कर इस महानगर की सड़कें छानता रहा था। कनॉट प्लेस के प्लाजा के पास से निकलती, फिरोजशाह रोड के उन दिनों के सन्नाटे में एक पेड़ से लगकर रोती बिट्टी मुझे बार-बार याद आती। मॉल रोड पर विश्वविद्यालय के कैफे मे बैठे नित्ती भाई और इरा का खयाल आता। निजामुद्दीन की मस्जिद के पीछे की बसावट ध्यान खींचती। मंडी हाउस में कहीं होने वाले रिहर्सलों में चेखव और स्ट्रिनबर्ग के नाटकों का ज़िक्र याद आता। मेरे लिए यह गालिबो-मीर की नहीं, निर्मल वर्मा की दिल्ली थी- विश्वविद्यालय से मंडी हाउस और निजामुद्दीन से कनॉट प्लेस तक अपनी तलाश में भटकती हुई एक यात्रा की दिल्ली।
तो शाम की ओर बढ़ती हुई उस दोपहर को मैं इस दिल्ली के वास्तुशिल्पी के साथ- अपने प्रिय लेखक निर्मल वर्मा के साथ- बैठा हुआ था। वह एक यादगार शाम थी- हम तीनों, निर्मल वर्मा, गगन गिल और मैं देर तक बात करते रहे। मेरे लिए समोसे लाए गए जो मिल कर खाए गए। फिर सड़क का पानी घटा, मैं नीचे उतरा, और बारिश से भरे उस दिन में अपने भीतर लबालब भरा लौटा।
..........
तब मैं दिल्ली नया-नया आया था। पांडव नगर के एक छोटे से घर में अपने तीन दोस्तों के साथ रहा करता था। अपना शहर छोड़कर एक नए शहर को अपना बनाने के संघर्ष में जो एक खुशनुमा सी उदास रुमानियत होती है, उससे हम सब भरे रहते। घर में एक दोस्त के लाए टेप रिकॉर्डर पर जगजीत सिंह की ग़ज़लें बजा करतीं और हम अपनी शामों को तरह-तरह के खयालों से आबाद रखते। महज 23 साल पहले का वह ज़माना याद कर अब हैरत होती है। वह मोबाइल फोन का दौर नहीं था। फोन मतलब वह लैंडलाइन होता था जिसके लिए तब भी नंबर लगा करते और एक नए शहर के संघर्षशील बाशिंदों के तौर पर फोन न सिर्फ़ हमारी कल्पना से बाहर था बल्कि शायद उसकी आज की तरह ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। फोन करने के लिए बिल्कुल अगल-बगल की सारी दुकानों पर सुविधा थी। बेशक, बाहर से फोन नहीं आ सकते थे. लेकिन हमें कौन फोन करता?
मगर यह सवाल मुझे तंग करता था। मैं नया-नया फ्रीलांसर था और इस ख़ुशफहमी में था कि अगर कोई संपादक मुझसे संपर्क करना चाहे तो किस नंबर पर करेगा। तो मैंने पड़ोस के एक दुकानदार का नंबर जुटा रखा था। वह उन दिनों बस फोन रिसीव करके जानकारी देने के तीन रुपये ले लिया करता था। मगर वे फोन महीने में एक-दो से ज़्याादा नहीं हुआ करते थे. इसलिए यह बहुत चुभने वाला अन्याय नहीं था। तो वही नंबर उस मुलाकात के बाद मैंने निर्मल वर्मा के घर भी छोड़ा था- ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि उनका फोन आएगा, मगर अपनी पेशेवर तैयारी के भ्रम में यह काम किया।
मगर एक दिन फोन आ गया। मुझे उस दुकानदार ने नाम याद करते हुए बताया- किसी गगन गिल का फोन है। मैंने तत्काल फोन किया। पता चला कि हिंदी में किताबों के एक प्रतिष्ठित प्रकाशक को एक संपादक की ज़रूरत है और निर्मल वर्मा और गगन गिल ने मेरा नाम प्रस्तावित किया है। मैं बेहद खुश था- इसलिए नहीं कि एक नौकरी की संंभावना खुली थी- ऐसी कई संभावनाओं के दरवाजे अपनी उस फ्रीलांसिंग के काल में मैं ख़ुद बंद कर चुका था। बस इसलिए कि यह ऐसी नौकरी होने जा रही है जिसके लिए निर्मल वर्मा ने मुझे योग्य माना। निर्मल वर्मा के कहने पर मैंने प्रकाशक से बात की। लेकिन अंततः बात कहीं नहीं पहुंची। प्रकाशक मुझे रखने को तैयार ते, मैं रहने को तैयार नहीं था क्योंकि पैसा मुझे मेरी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं मिल रहा था। मैं फ्रीलांसिंग में कहीं ज़्यादा पैसे कमा लिया करता था। निर्मल वर्मा को मैंने जब यह बताया तो वे दुखी हुए। उन्होंने यह बात मानी कि वाकई प्रकाशक की पेशकश पेशेवर नहीं है।
..........
बहरहाल, आने वाले वर्षों में मुझे नौकरी मिल गई। 1996 में मैं जनसत्ता में कनिष्ठ सहायक संपादक हो चुका था। यह ख़बर हमने आपस में साझा की। वे खुश हुए। इसके बाद की मुलाकातें किन्हीं कार्यक्रमों में होने वाली मुलाकातें रहीं। कभी-कभार मेरे कुछ लेखों और संपादकीयों पर भी उन्होंने प्रशंसा के अंदाज़ में टिप्पणी की। इस बीच उनका उपन्यास 'अंतिम अरण्य' भी प्रकाशित हुआ। पता नहीं क्यों मुझे इस उपन्यास से एक अजब सी हूक होती रही। लगा कि कभी मेरी कल्पनाओं का युवा लेखक उम्र के उस पड़ाव की कहानी लिख रहा है जहां ठहर कर पीछे देखने के दिन शुरू हो जाते हैं। इत्तिफाक से लगभग उन्हीं दिनों कृष्णा सोबती का 'समय सरगम' भी प्रकाशित हुआ था। इन दोनों उपन्यासों में वार्धक्य और मृत्यु की जो छाया थी, वह मुझे हिंदी के बदलते दौर की पहचान की तरह याद आती रही। 'अंतिम अरण्य' पर मैंने दूरदर्शन के एक कार्यक्रम के लिए नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी के साथ बातचीत की थी। इसी आसपास निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ सम्मान देने की घोषणा हुई। हालांकि इस सम्मान में निर्मल वर्मा के साथ पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह भी साझा कर रहे थे। गुरदयाल सिंह भी मेरे प्रिय उपन्यासकारों में रहे। ख़ासकर उनका उपन्यास परसा मुझे बेहद पसंद था और मैंने हंस में इसकी एक समीक्षा भी लिखी थी। लेकिन जनसत्ता मेें इस पुरस्कार पर बहस चली, यह सवाल भी उठा कि कहीं यह निर्मल वर्मा के साथ अन्याय तो नहीं।
........
इन सारी साहित्यिक-संस्कृतिक हलचलों और बहसों के बीच निर्मल वर्मा से बातचीत होती रही, लेकिन एक यादगार मुलाकात का बहाना इसके बाद निकला। साल 2000 में अचानक मेरे पास ज़ी टीवी से फोन आया। आकृता नाम की एक प्रोड्यूसर ने फोन किया था। ज़ी टीवी वाले अपनी एक प्रतिष्ठित शृंखला 'विज़न बियॉन्ड फ़िफ्टी' के लिए निर्मल वर्मा का एक इंटरव्यू करना चाहते थे। आकृता ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं यह इंटरव्यू लूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरा नाम आकृता को किसने सुझाया था। ये वे दिन थे जब निर्मल वर्मा पर उनकी वैचारिकता को लेकर लगातार हमले हो रहे थे। यह आरोप लगाया जा रहा था कि वे भारतीय जनता पार्टी के क़रीब हैं और आडवाणी के पक्ष में उन्होंने अपील की है। दूसरी तरफ निर्मल वर्मा अपनी जानी-पहचानी मृदु मगर दो टूक शैली में अपने विरोधियों का प्रत्युत्तर दे रहे थे। इसमें शक नहीं कि वामपंथ विरोध की उनकी वैचारिकी में बहुत सारे तत्व ऐसे थे जो दक्षिणपंथी राजनीति को अपने लिए उपयोगी लग सकते थे, लेकिन यह सच है कि राजनीति दक्षिण की हो या वाम की- दोनों का उस गहन वैचारिकता से कोई सरोकार नहीं रह गया है जो उनके लेखकों के लेखन में दिखती है। निर्मल वर्मा का अपना पक्ष जो भी हो- बीजेपी के लिए वे शोभा और इस्तेमाल की वस्तु भर थे- निर्मल की वैचारिकी से उनको लेना-देना नहीं था। खैर, उनसे इंटरव्यू लेने से पहले मैंने तय किया कि अगर असुविधाजनक भी हों तो ये सवाल मैं पूछूंगा। मैंने पूछा और उन्होंने शालीन दृढ़ता से इसका उत्तर दिया- इस बात से इनकार करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल को लेकर उन्होंने कोई अपील जारी नहीं की है।
इस इंटरव्यू से जुड़़ी एक बात और याद हैं। यह इंटरव्यू ज़ी टीवी पर उस दिन आया जब बिहार चुनावों के नतीजे आ रहे थे। अचानक वह बहुत सारे लोगों द्वारा देख लिया गया। मुझे कई फोन आए, ज्यादातर लोग उसे एक समृद्ध इंटरव्यू मान रहे थे। लेकिन राजेंद्र यादव ने कहा कि मुझे कुछ और सख्त सवाल करने चाहिए थे। मैंने कहा कि एक पेशेवर साक्षात्कारकर्ता की तरह किसी एक सवाल पर जितनी बार मुझे कुरेदना चाहिए था, उतना भर मैंने किया। मेरा काम उनका पक्ष जानना था, अपनी राय के हिसाब से सच उगलवाना नहीं। राजेंद्र यादव अपनी आदत के मुताबिक इस पर ठठा कर हंसे।
.........
इंटरव्यू वाले दिन एक और मार्मिक प्रसंग घटा था। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद ज़ी टीवी की टीम निकल गई। मुझे निर्मल वर्मा ने रोक लिया- 'गगन बाहर गई हुई हैं। आप रुकिए हम लोग गप करेंगे। मैं आपको अपने हाथ की बनी चाय पिलाता हूं।' मेरे लिए ना करने के सवाल ही नहीं था। तो हम कम से कम दो घंटे बैठे रहे, निर्मल जी ने एक बार नहीं, दो बार चाय बनाई। एक लंबे से कप से उठती हुई वह भाप जैसे उस पूरे कमरे की ऊष्मा को प्रतिबिंबित कर रही थी। वे अपनी मृदु-मंथर शैली में धीरे-धीरे बोल-सुन रहे थे और मुझे उनकी कहानियों की कुहरीली सुबहें-शामें याद आ रही थीं। इस बातचीत के दौरान अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ज़ी टीवी वाले इस इंटरव्यू के लिए उन्हें कोई भुगतान करेंगे? मैंने उन्हें बताया कि मुझे तो वे भुगतान करेंगे, उनको करेंगे या नहीं, यह नहीं मालूम। दरअसल फ्रीलांसिंग के दिनों की बची-खुची आदत के तहत मैंने आकृता से पहला सवाल यही पूछा था कि क्या इस इंटरव्यू के लिए ज़ी टीवी वाले मुझे कोई भुगतान करेंगे। उसने बताया था कि आने-जाने की व्यवस्था के अलावा मुझे और भी पैसे मिलेंगे। निर्मल जी ने कहा कि कायदे से भुगतान तो उन्हें भी होना चाहिए। मैंने सहमति जताई। करीब 15 दिन बाद मुझे ढाई हज़ार रुपये का चेक आया। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैने तत्काल निर्मल वर्मा को फोन कर जानकारी दी। फिर मैंने आकृता से पूछा। आकृता ने बताया कि जो इटरव्यू करता है, उसको भुगतान होता है, जिसका इंटरव्यू लिया जाता है, वह तो बड़ा आदमी माना जाता है। निर्मल वर्मा को मैंने बताया तो वे मुस्कुरा भर दिए।
अब मैं सोचता हूं कि हिंदी के इतने बड़े लेखक को एक इंटरव्यू के लिए भुगतान की अपेक्षा क्यों करनी पड़ती है? हिंदी का समाज उसे अपनी किताबों से इतने पैसे क्यों नहीं देता कि वह पुरस्कारों और ऐसे भुगतानों का मोहताज रहे? दरअसल वह एक करुण दृश्य था जिसे निर्मल वर्मा के व्यक्तित्व की उदात्तता ने ढंके रखा। निस्संदेह वे गरीब नहीं थे और दिल्ली में सलीके का मध्यवर्गीय जीवन जी सके, लेकिन हममें से कितने लोग हैं जो किसी नौकरी के बिना, सिर्फ लिखकर गुजारा करने का हौसला रख सकें?
.......
ये छोटे-छोटे सुख थे जो निर्मल वर्मा की टुकड़ा-टुकड़ा मुलाकातों से हासिल होते रहे- हमारे हिस्से का एक चिथड़ा सुख- जो दिल्ली में रहने के बहुत सारे दुखों पर भारी पड़ा। 2002 के बाद जब मैं एनडीटीवी चला आया तो एक नए माध्यम की आंधी में जैसे सारे पुराने पुल टूट गए। उन्हीं दिनों राजेंद्र यादव ने कभी अपने विनोदी लहजे में यह शिकायत भी की- लोग अल्लाह को प्यारे होते हैं, तुम टीवी को प्यारे हो गए हो। लेकिन बीच-बीच में किन्हीं समारोहों और आयोजनों में निर्मल जी पुरानी आत्मीयता से मिलते और मेरा हालचाल लेते। कायदे की आखिरी भेंट शायद 2003 में ओम थानवी के घर हुई जब उन्होंने जनसत्ता से मंगलेश डबराल और मेरी विदाई के उपलक्ष्य में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसमें निर्मल वर्मा और गगन गिल के अलाव राजेंद्र यादव, कुंवरनारायण और विष्णु खरे सहित हिंदी के कई मूर्द्धन्य लेखक शामिल थे। बातचीत इसके बाद भी चलती रही।
लेकिन एक दिन सब कुछ रुक गया। यह मालूम था कि निर्मल वर्मा बीमार हैं। अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन कभी उनको देखने गया नहीं। दूसरों से ख़बर लेता रहा। 25 अक्टूबर 2005 को इसकी भी ज़रूरत नहीं रह गई। निर्मल वर्मा अपने अंतिम अरण्य के पार चले गए। दिल्ली के सह विकास अपार्टमेंट के उनके घर से लेकर लोदी रोड के शवदाहगृह तक शोकाकुल लेखकों-पत्रकारों और पाठकों का हुजूम बताता रहा कि लोग उनको कितनी शिद्दत से चाहते थे। एनडीटीवी इंडिया पर हमने उन पर आधे घंटे के कार्यक्रम का कार्यक्रम भी किया। अपने भीतर उमड़ते-घुमड़ते दुख को स्थगित रख कर मैं वह सब जोड़ने-संजोने की कोशिश करता रहा जो निर्मल जी स्मृति के तौर पर मेरे लिए छोड़ गए थे। यह बहुत छोटी सी पोटली है, लेकिन बहुत बेशक़ीमती है। उस दिन अपने न्यूज़ रूम में खड़ा मैं चारों तरफ लगे टीवी सेट्स को देख रहा था जिन पर निर्मल वर्मा की श्रद्धांजलियां जारी थीं। अचानक किसी ने मुझे कहा, अरे यहां तो आप दिख रहे हैं। मेरी नज़र पड़ी। ज़ी टीवी पर मैं निर्मल वर्मा से सवाल पूछ रहा था। यह वही पुुराना इंटरव्यू था जो इस मौके पर चैनल ने रिपीट किया। जाते-जाते जैसे एक संवाद को पुनर्जीवित कर गए निर्मल वर्मा।
भाग प्रियदर्शन जी की कलम से 'निर्मल वर्मा' जी पर कुछ और ....
--------
निर्मल वर्मा को लेकर चर्चा जारी है। तीन साल पहले शंपा शाह के कहने पर 'कथादेश' के निर्मल वर्मा विशेषांक के लिए मैंने अपने पसंदीदा दो बिल्कुल अलग तरह के उपन्यासों को लेकर एक कुछ बेढब सी टिप्पणी लिखी थी। मैंने यह समझने की कोशिश की थी कि दो बिल्कुल भिन्न तरह के उपन्यास 'एक चिथड़ा सुख' और 'परती परिकथा' मुझे समान रूप से प्रिया क्यों हैं? हालांकि लेख के केंद्र में 'एक चिथड़ा सुख' ही था। फिर यह लेख साझा कर रहा हूं।
यह एक चिथड़ा सुख की तलाश नहीं है
जिन दो उपन्यासों ने एक दौर में मेरे भीतर अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी- और जिन्हें बार-बार पढ़ने की इच्छा होती है- उनमें एक फणीश्वर नाथ रेणु का ‘परती परिकथा’ है और दूसरा निर्मल वर्मा का ‘एक चिथड़ा सुख’। हालांकि ये दोनों एक-दूसरे से नितांत भिन्न आस्वाद की कृतियां हैं- एक में आंचलिक आभा है तो दूसरे में महानगरीय वैभव। एक की कथा पूर्णिया के परानपुर नाम के पिछड़े गांव में घूमती है तो दूसरे के चरित्र दिल्ली के संभ्रांत ठिकानों में भटकते हैं। एक में सामूहिकता के उत्सव के बीच भविष्य की कल्पना है तो दूसरे में अपनी एकांतिकता की अपने वर्तमान से मुठभेड़ का यथार्थ। एक में पचास के दशक में देखा गया विकास का नेहरूवादी सपना है तो दूसरे में ऐसा कोई सपना नहीं है, बस एक कशमकश है और एक बेचैन पड़ताल- एक चिथड़ा सुख की स्मृति की, या उसकी तलाश की।
लेकिन दो नितांत भिन्न कृतियों में वह कौन सी एक समान चीज़ होती है जो किसी पाठक को फिर भी आकृष्ट करती है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। इस पर विचार करते हुए मुझे यह खयाल आता है कि रेणु और निर्मल वर्मा दोनों व्यक्ति के अंतर्जगत के भी अद्भुत चितेरे हैं। बल्कि अपनी जड़ों से टूटने और फिर उन्हें खोजने की कसक उनके किरदारों को भटकाती रहती है। ‘परती-परिकथा’ का नायक जित्तन मिश्र ऐसा ही किरदार है- देश और समाज को बदलने की चाहत और इसे बदलने निकले लोगों की हक़ीक़त उसे जड़ों से भी काट देती है और बाक़ी दुनिया से भी। अलग-अलग ग्राम प्रांतरों में घूमते हुए, सितार बजाने से लेकर पत्रकारिता करते हुए, अंततः वह जड़ों की तलाश में गांव लौटा है। गांव वाले उसे पागल कहते हैं। इरावती भी विभाजन की चोट खाई भटकती हुई एक लड़की है जो अपने परती-पुत्तर को खोज रही है। बल्कि विकास की हवा में गांव की चूलें भी उखड़ गई हैं। सर्वे की आंधी में सब उड़ रहे हैं- रिश्ते-नाते, भरोसा और सरोकार और वह जीवन जो सामूहिकता से बना है। इस टूटन के बीच अलग-अलग चरित्र तरह-तरह की छटपटाहटों से भरे हैं- ताजमनी, मलारी, लुत्तो- सबके अपने-अपने दुख हैं- जितने सामाजिक, उतने ही निजी भी-बल्कि सारी खरोचें देह से ज़्यादा चेतना पर पड़ी हुई हैं। अपनी सारी आंचलिकता और सामाजिकता के बावजूद यह व्यक्तिगत छटपटाहट न होती तो ‘परती परिकथा’ हमारे भीतर किसी ‘तीरे नीमकश’ की तरह धंसी हुई न होती।
निर्मल वर्मा के यहां तो जैसे सारे के सारे चरित्र अपनी जड़ों से उखड़े हुए हैं। इलाहाबाद से आई बिट्टी अपनी बेख़याली में दिल्ली के रंगमंच में अपना ठिकाना खोज रही है। उसका भाई दर्शक भी है, भोक्ता भी और एक तरह से लेखक भी- जो सबकुछ देख और झेल रहा है।
इस मोड़ पर एक बात और विचार करने लायक है। यह जो जड़ों से कटे रहने की त्रासदी है, क्या वह कोई निजी त्रासदी है जो किन्हीं चरित्रों की आंतरिक उलझनों या मजबूरियों से पैदा हुई है? दरअसल ठीक से देखें तो अपने दूसरे हिस्से में बीसवीं सदी विस्थापित लोगों की सदी है। तरह-तरह के दबावों में गांव-घर छूटे हैं और नए इलाकों में अपनी पुरानी पहचान खोजते लोग यह जान कर ठिठके हुए हैं कि वे तो वे नहीं रहे जो वे हुआ करते थे।
निर्मल वर्मा इस सामाजिक त्रासदी के बीच पैदा हुई व्यक्तिगत विडंबना को लगभग एक अस्तित्ववादी बेचैनी के चरम पर ले जाते हैं। 'एक चिथड़ा सुख' का पाठ इसलिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। इस अविस्मरणीयता की वजहें और भी हैं। इन वजहों में उतरते हुए हम यह भी समझ पाते हैं कि बड़ी कृतियां अंततः अद्वितीय ढंग से मौलिक होती हैं, कि ‘परती-परिकथा’ और ‘एक चिथड़ा सुख’ के बीच के समान तत्वों की खोज या उनकी प्राप्ति के बावजूद दोनों एक-दूसरे से नितांत भिन्न रचनाएं हैं।
निर्मल वर्मा के चरित्र जैसे आधुनिक सभ्यता के बियाबान में छटपटाते चरित्र हैं। वे सब ख़ुद को खोज रहे हैं, अपनी जगह खोज रहे हैं। ‘एक चिथड़ा सुख’ की नायिका बिट्टी इलाहाबाद से दिल्ली आई है। वह रंगमंच के अलग-अलग चरित्रों को जीती हुई जैसे अपने ही जीवन के मायने तलाश रही है। उसे एहसास है कि कुछ है जो खो गया है। इस एहसास को निर्मल वर्मा जिस सहजता और संवेदनशीलता के साथ उपन्यास में जगह देते हैं, वह भी दृष्टव्य है। बिट्टी और उसका कजिन सोने से पहले चुप्पी और संवाद के बीच आवाजाही कर रहे हैं- कुछ स्मृतियों का सिरा पकड़ कर और कुछ वर्तमान के दुखों के रेशे खोलते हुए। निर्मल वर्मा ने इसका वर्णन कुछ इस तरह किया है:
"कुछ देर बाद स्लीपिंग बैग हिला, मुंह बाहर निकला, छोटी सी आवाज़ आई, 'मुन्नू?'
'हूं', उसने करवट ली।
'तुम क्या सोचते हो, अगर वह ज़िंदा होतीं, तो मुझसे बहुत निराश हो जातीं?'
'बिट्टी,' उसका स्वर न जाने क्यों बहुत रुंधा सा हो आया। 'वह तुम्हें बहुत मानती थीं।'
'मुझे नहीं... वह लड़की कोई और थी।'
'और तुम... तुम कौन हो?'
'मैं'...-उसने बहुत धीमे से कहा। 'मैं उसे ही ढूंढ़ने दिल्ली आई थी।' "
यह त्रासदी है जो उपन्यास में जैसे हर किसी के साथ घटित हो रही है। लंदन से हिंदुस्तान के लिए चली इरा पा रही है कि वह हिंदुस्तान में नहीं थिएटर में है। वह लौट जाना चाहती है। यह भी साफ नहीं है कि वह क्यों आई थी। क्या उसे शादीशुदा नित्ती भाई का प्रेम खींच लाया था? और नित्ती भाई? वे जैसे खुद कई दुनियाओं में, कई किरदारों में बंटे हुए हैं।
इसी तरह डैरी हैं- दिल्ली में एक रईस बाप के बेटे जो बिहार से भटकते हुए रंगमंच में चेखव और स्ट्रिनबर्ग के बीच भटक रहे हैं।
निर्मल वर्मा ने यह कहानी बहुत मनोयोग से लिखी है। कुल चार-पांच मुख्य किरदारों के बीच घूमती इस कहानी में छठा किरदार दिल्ली नाम का वह शहर है जहां ये सब अपने-अपने हिस्से की भूमिकाएं खोजने इकट्ठा हुए हैं। वैसे तो दिल्ली बहुत सारे लोगों की है- एक दौर में हुए बादशाहों की है, एक दौर में हुए शायरों की है, लेकिन एक दिल्ली निर्मल वर्मा भी बनाते हैं- वह दिल्ली जहां सब अपनी-अपनी पहचान और अपना-अपना मक़सद ढूढ़ने आए हैं। मंडी हाउस, बाराखंबा रोड, निजामुद्दीन, ओडियन सिनेमा, माल रोड- ये दिल्ली के नक़्शे पर दर्ज जगहों के नाम भर नहीं हैं, निर्मल वर्मा के उपन्यास के भीतर इनके किरदारों के वे ठिकाने भी हैं जहां से गुज़रते हुए ये सब खुद को बार-बार खो देते, खोजते और फिर पहचानने की कोशिश करते हैं।
यही वह मोड़ है जहां ‘एक चिथड़ा सुख’ फिर से ‘परती परिकथा’ की याद दिलाता है। यह सवाल पूछने की इच्छा होती है कि अगर ‘परती-परिकथा’ एक आंचलिक उपन्यास है तो ‘एक चिथड़ा सुख’ क्यों नहीं। क्या इसलिए कि दिल्ली देहात जैसी नहीं लगती और इस उपन्यास के किरदारों की भाषा में वह भदेसपन नहीं है जिसे हम अमूमन आंचलिकता के साथ जोड़ने के आदी हो गए हैं? लेकिन अगर अपने इस अभ्यास को कुछ देर के लिए स्थगित कर सकें तो हम पाएंगे कि निर्मल वर्मा का उपन्यास भी ठेठ आंचलिक उपन्यास है- बस इसलिए नहीं कि इसमें दिल्ली का भूगोल या नक़्शा मिलता है, बल्कि इसलिए कि यह उपन्यास बस दिल्ली में ही घट सकता था- एक ऐसे महानगर में जो बाहर से इतना समृद्ध और संवेदनशील दिखाई पड़ता है कि किसी को अपने खोए हुए वजूद की तलाश के लिए बुला सकता है और भीतर से इतना तंगदिल और खोखला साबित होता है कि वह हर किसी को ख़ाली हाथ लौटा सकता है।
लेकिन क्या वाकई यही सच है? क्या निर्मल वर्मा ने जो दिल्ली रची है वह इतनी हृदयहीन है कि सबको ख़ाली हाथ लौटा देती है? इस मोड़ पर निर्मल वर्मा फिर उस्ताद लेखक साबित होते हैं। यह उनके लेखन का करिश्मा है कि यह दिल्ली जैसे हमारे भीतर भी धंसती-बसती चली जाती है, हम इस दिल्ली से मोहब्बत करने लग जाते हैं। दरअसल यहां पता चलता है कि इस शहर ने आपको जितना ख़ाली कर दिया है उससे कहीं ज्यादा भर दिया है। बिट्टी के नाटक का मंचन छोड़कर मुन्नू जब इलाहाबाद लौटेगा तो एक भिन्न व्यक्ति होगा जिसके भीतर बहुत सारी यादों का एक आबाद संसार होगा, जीवन की बहुत गहरी समझ होगी, सुख और दुख उसके जीवन में यंत्रवत आएंगे-जाएंगे नहीं, बल्कि उन्हें वह ठीक से महसूस कर सकेगा, बेशक वह उन्हें बार-बार खोजता और खोता भी रहेगा। अंततः निर्मल वर्मा की दिल्ली वह किरदार है जो आपको चोट भी पहुंचाती है और सहारा भी देती है। उसकी वजह से जीवन व्यर्थ लगता है और उसी के साए तले जीवन के मायने खोजने की व्याकुलता भी पैदा होती है। अब 'एक चिथड़ा सुख' को दिल्ली के संदर्भ में निर्मल वर्मा का आंचलिक उपन्यास न कहें तो क्या कहें।
रंगमंच वह धागा है जो इस पूरी कथा को पिरो रहा है। निर्मल इसी रंगमंच की मार्फ़त कला में जीवन के पुनर्वास का स्वप्न भी देखते हैं और उसके बिखरते जाने की सच्चाई भी महसूस करते हैं। 500 बरस पहले शेक्सपियर का मैकबेथ अपनी छटपटाहट में चीखता है- ‘जीवन एक चलती हुई छाया है, एक कमज़ोर कलाकार जो अपने तय समय तक मंच पर ऐंठती-इठलाती है और फिर किसी को सुनाई नहीं पड़ती। यह किसी मूर्ख द्वारा सुनाई जा रही कथा है जिसमें शोर और हंगामा बहुत है, लेकिन अर्थ नहीं।‘
लेकिन जीवन के इस विराट आख्यान के समानांतर निर्मल के चरित्रों की छटपटाहट मैकबेथ के इस वक्तव्य की उदात्तता से कुछ भिन्न है। बल्कि शायद वे ‘मर्चेंट ऑफ वेनिस’ के ऐंटोनियो की याद दिलाते हैं- ‘मैं दुनिया को एक रंगमंच की तरह देखता हूं ग्रैटियानो जिसमें हर कोई अपनी भूमिका अदा कर रहा है, और मेरे हिस्से एक उदास किरदार है।‘ यह उदासी निचाट अकेलेपन से, या किसी अन्य संशय से पैदा हुई उदासी नहीं है- यह फिर इस आकुलता से जन्मी है कि उनके भीतर कुछ है जो बाहर नहीं आ रहा है, कुछ है जो अव्यक्त रह जा रहा है, कुछ है जिसे दूसरे ढंग से जिया जाना था। रिहर्सल के दौरान वे कुछ से कुछ हो जाते हैं। मुन्नू न बिट्टी को ठीक से पहचान पाता है न इरा को। उसे लगता है- वे तो कोई और हैं जो बिल्कुल एक अलग जीवन जी रहे हैं।
लेकिन इस कथा का असली नायक किशोर मुन्नू है- बिट्टी का कजिन- जिसे मां ने मरने से पहले एक डायरी दी है, साथ में हिदायत भी- कि जो देखना वही लिखना। लेकिन क्या जो दिखाई पड़ता है वही सच होता है? क्या दृश्य के भीतर बहुत सारे अदृश्य नहीं होते हैं? और जो अदृश्य होता है क्या वह भी तरह-तरह के दृश्यों में बंटा नहीं होता? मुन्नू कहीं भोक्ता है कहीं दर्शक और कहीं सब कुछ का लेखक- वही है जो उपन्यास के भीतर चल रहा नाटक भी देख रहा है और ज़िंदगी के भीतर चल रहा नाटक भी। मुन्नू जैसे लेखक की आंख से इसे देख रहा है- जीवन की समूची गतिमयता को, उसके एक-एक क्षण में छुपी निरीहता को। वह लिखता है- ‘तुम देखे को न समझो, यह बात दूसरी है, लेकिन एक बार देख लेने पर दुनिया एक कीड़े की तरह सुई की नोक पर बिंध जाती है, तिलमिलाती है, लेकिन कोई उसे छुड़ा नहीं सकता। देखना तभी ख़त्म होता है, जब मरना होता है, और मरने पर भी आंखें खुली रहती हैं- जैसे मां की आंखें थीं- कांच के दो कंचे- जिन पर दुनिया एक पथराई छाया की तरह चिपकी रहती है।‘ कहना न होगा, दुनिया को इस तरह की सूक्ष्मता के साथ देखते हुए निर्मल वर्मा लगभग महाकाव्यात्मक हो उठते हैं।
अपने पसंदीदा लेखकों में निर्मल वर्मा एकाधिक बार टॉमसमॉन जेम्स ज्वायस आदि का ज़िक्र करते रहे हैं। लेकिन ‘एक चिथड़ा सुख’ पढ़ते हुए मुझे सबसे ज़्यादा अल्बेयर कामू की याद आती है- उसके ‘आउटसाइडर’ की। कामू का नायक लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के मारे यूरोप में पैदा हुई व्यापक अनास्था की संतान था जिसके लिए जीवन के मायने ही मायने नहीं रखते थे। निर्मल वर्मा के किरदारों की यातना लगभग वैसी ही वेधक है, लेकिन वह एक दूसरी त्रासदी से पैदा हुई है। वह शायद उस अकेलेपन से पैदा हुई है जो इस विस्थापित सभ्यता का अपरिहार्य सह-उत्पाद है।
क्या निर्मल या उनके किरदार इस अकेलेपन से मुठभेड़ की कोई राह प्रस्तावित करते हैं? क्या उनमें किसी मुक्ति की कामना है? इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। लेकिन एक बात समझ में आती है- डैरी से नित्ती भाई तक, इरावती और बिट्टी से उसके कजिन तक- जैसे सब यह समझ रहे हैं कि जीवन तलाश में है, प्राप्ति में नहीं, शायद इस तलाश से कुछ लम्हों की निजात में भी है जब बिट्टी की बरसाती पर सब जमा होते हैं, रिकॉर्ड बजाते हैं, बीयर पीते हैं, बहस करते हैं और कभी लड़-झगड़ कर, एक दूसरे को चोट पहुंचा कर, फिर पछताने और सहलाने का ज़रूरी काम भी करते हैं। अगर वह छटपटाहट निकाल दी जाए जो इन सबको भटका रही है तो फिर एक बड़ा शून्य बचेगा, जिसमें शेक्सपियर के मुताबिक शोर और हंगामा भले हो, लेकिन अर्थ नहीं होगा। सारी व्यर्थता के बीच यह अर्थ अनुभव करके मुन्नू लौट रहा है। उसे अब नाटक नहीं देखना है जब वह मंचित होने वाला है। अर्थ और व्यर्थ के बीच घूमती, इस कुछ भटकी हुई टिप्पणी के बीच उपन्यास के आख़िरी हिस्से का एक लंबा उद्धरण देने की इच्छा हो रही है- ‘नहीं, सच, कहीं जाने के लिए टिकट का होना ज़रूरी है। यह एक तरह का सिग्नल है जैसे घड़ी का होना, डायरी का होना, कैलेंडर का होना- वरना एक रात हमेशा के लिए रात रहेगी, एक शहर हमेशा के लिए एक शहर, एक मृत्यु हमेशा के लिए एक मृत्यु, उसके जाने के बाद भी बारहखंबा रोड की सड़क चलती रहेगी, मंडी हाउस के आगे वह पेड़ खड़ा रहेगा जिसे पकड़ कर एक रात अंधेरे में नित्ती भाई खड़े रहे थे; सप्रू हाउस की झाड़ियां, सिगरेट की दुकान, लहराते पेड़ ज्यों के त्यों खड़े रहेंगे और बरसों बाद जब कोई इस सड़क से गुज़रेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि यहां बहुत पहले एक लड़की एक छोटे से लड़के के साथ जाती थी और वह लड़का इलाहाबाद से आया था और वह लड़की रोड-साइन के तख़्ते पर सिर रखकर रोई थी।‘
इस उपन्यास को पढ़ना एक अप्रतिम कथा-शिल्पी की अंगुली पकड़ कर बहुत गहरी और वेधक मार्मिकता के साथ जीवन की कई परतों को पहचानना है।
—
प्रियदर्शन की स्मृति से
| व्हाट्सएप शेयर |
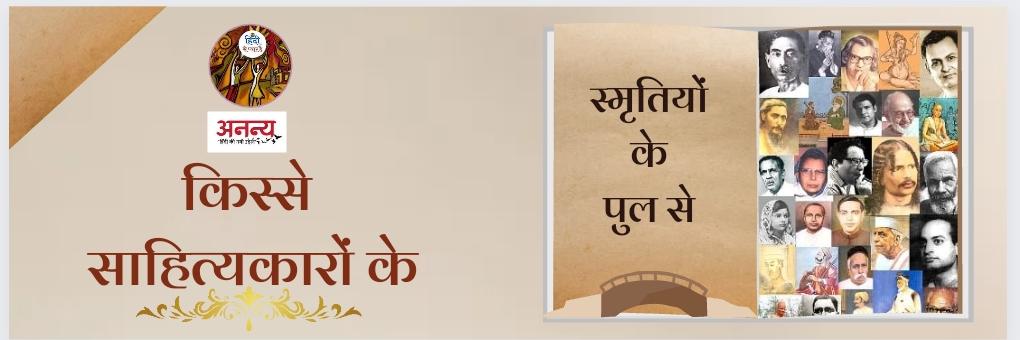
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें