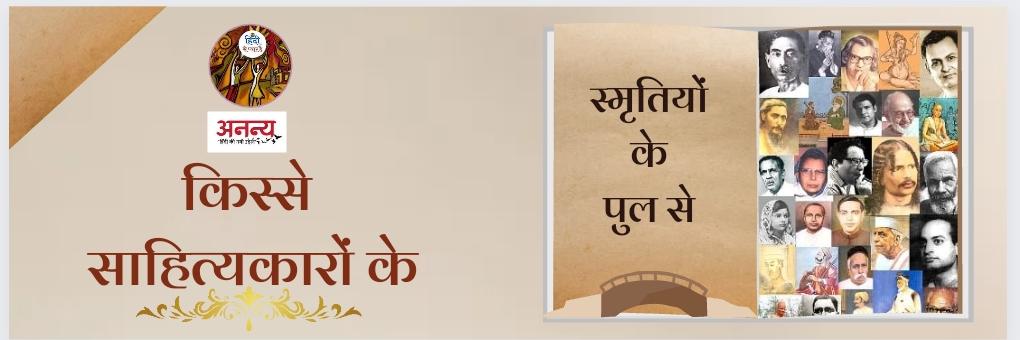मूर्खों के हाथ पड़ा साइंस - सिनेमा
बंबई की एक फिल्म कंपनी मुझे बुला रही है। तनख्वाह की बात नहीं, ठेके की बात है। आठ हजार रुपए सालाना पर। मैं इस हालात पर पहुँच गया हूँ, जब मुझको इसके सिवा कोई चारा भी नहीं रह गया है कि या तो चला जाऊँ या अपने नॉवेल को बाजार में बेचूँ। अजंता सिनेटोन कंपनी वाले हाज़िरी की कोई क़ैद नहीं रखते। मैं जो चाहूँ लिखूँ, जहाँ चाहे चला जाऊँ...। वहाँ साल भर रहने के बाद ऐसा अनुबंध कर लूँगा कि यहीं बनारस में बैठे-बैठे मैं चार कहानियाँ लिख दिया करूँगा और चार-पाँच हजार रुपए मिल जाया करेंगे, जिससे 'जागरण' और 'हंस' दोनों मजे से चलेंगे और पैसे की तकलीफ जाती रहेगी।
मैं पहली जून 1934 में बंबई चला गया। उस कंपनी से अनुबंध कर लिया। साल भर में छह कहानियाँ उनको देना होंगी। पत्रिकाओं से लगातार नुकसान हो रहा था, बुक सेलर से रुपए वसूल न होते थे। काग़ज़ वगैरह का भाव बढ़ता जा रहा था, सो मजबूर होकर अनुबंध कर लिया। छह कहानियां लिखना मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्टर के मशविरे से लिखना ज़रूरी है। क्या चीज़ फिल्म के लिए ज़रूरी है, इसका बेहतर फैसला वही कर सकते हैं।
मैं जिस इरादे से बंबई आया था, उसमें से एक भी पूरा होता नज़र नहीं आया। प्रोड्यूसर जिस तरह की कहानी पर फिल्म बनाते रहे हैं, उस लीक से वे नहीं हट सकते। बेहूदा मज़ाक़ को तमाशे की जान समझते हैं। इनका विश्वास अनोखा है। राजा-रानी, वज़ीरों की साज़िशें, नकली लड़ाई, चुंबन यही उनका मक़सद है। मैंने सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं, जिन्हें शिक्षित वर्ग भी देखना चाहता है, लेकिन इनको फिल्म बनाते हुए संदेह होता है कि यह चले या न चले...। अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पटकथा लिखें, तो फिल्मों में जान बढ़ जाए, मगर आप तो जानते हैं, फिल्म निम्न वर्ग के दर्शकों के लिए होती है, वो अच्छी पटकथा की कद्र नहीं कर सकते। मगर खैर! ये लोग कद्र न करें, समझने वाले तो करते हैं। 'बाजारे हुस्न' की मिट्टी पलीद कर दी, 'मिल मज़दूर' अलबत्ता कुछ अच्छी रही। यह साल (1934) तो पूरा करना ही है। क़र्ज़दार हो गया था, क़र्ज़ पट जाएगा। और कोई फायदा नहीं हुआ, तो अपने पुराने अड्डे पर जा बैठूँगा। वहाँ दौलत नहीं है, मगर सुकून जरूर है। यहाँ तो मालूम होता है कि ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ।
सिनेमा के माध्यम से पश्चिम की सारी बेहूदगी हमारे अंदर दाखिल की जा रही है और हम बेबस हैं। पब्लिक में अच्छे-बुरे की समझ नहीं है। आप अखबार में कितनी ही फरियाद कीजिए, वह बेकार है। अख़बार वाले भी साफ़गोई से काम नहीं लेते। जब एक्ट्रेस और एक्टरों की तस्वीरें धड़ाधड़ छपें और नौजवानों पर जो असर नज़र आ रहा है, इन अखबारों की बदौलत, उसमें दिन-ब-दिन तरक्की हो रही है।
मेरा फैसला हो गया। 25 मार्च 1935 को अपने शहर बनारस जा रहा हूँ। अजंता कंपनी अपना करोबार बंद कर रही है। मेरा अनुबंध तो साल भर का था और अभी तीन महीने बाकी हैं, लेकिन मैं उनकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता। महज इसलिए रुका हुआ हूँ कि फरवरी और मार्च की रकम वसूल हो जाए और जाकर फिर अपने साहित्य के काम में व्यस्त हो जाऊँगा। आजकल मेरी सेहत निहायत कमजोर हो रही है। लिखना-पढ़ना छोड़ दिया है। एक साहित्यकार के लिए सिनेमा में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इस लाइन में इसलिए आया था कि अपनी आर्थिक स्थिति सुधार जाएगी, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मैं धोखे में था और फिर साहित्य की तरफ लौट रहा हूँ। साहित्य, शायरी और दूसरी कलाओं का मकसद सदा यही रहा है कि आदमी में जो बुराइयाँ हैं, उन्हें मिटाकर अच्छाइयाँ जगाई जाएं। उसकी बुरी प्रवृत्ति को दबाकर या मिटाकर कोमल, नर्म, नाज़ुक और पवित्र जज़्बात को बेदार (जाग्रत) किया जाए। अगर सिनेमा इसी आदर्श को सामने रखकर फिल्में पेश करता, तो आज वह दुनिया को आगे बढ़ाने में सबसे शक्तिशाली सिद्ध होता।
जिस जमाने में बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन था, अधिकतर सिनेमा हॉल खाली रहते थे और उन दिनों जो फिल्में प्रदर्शित हुईं, वो नाकामयाब रहीं। इसका सबब इसके सिवा और क्या हो सकता है, कि अवाम के बारे में जो विचार है कि वो मारकाट और सनसनी पैदा करने वाली फिल्मों को ही पसंद करती है, महज भ्रम है। अवाम उनके कमाल के क़सीदे गाए जाए, तो क्यों न हमारे नौजवान पर इसका असर होगा। साइंस एक रहमत है, मगर मूर्खों के हाथों में पड़ कर लानत हो रही है। जिन हाथों में फिल्म की क़िस्मत है, वो बदकिस्मती से इसे इंडस्ट्री समझ बैठे हैं। समाज में सुधार के बजाय शोषण कर रहे हैं। नग्नता, क़त्ल, खून और जुर्म की वारदातें, मारपीट ही इस इंडस्ट्री के औजार हैं और इसी से वह इंसानियत का खून कर रहे हैं।
मैं, बंबई में ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। यहाँ की आबोहवा और फ़िज़ा दोनों ही मेरे माफ़िक़ नहीं हैं। हममिज़ाज आदमी नहीं मिलता, महज ज़िंदगी में एक नया तजुर्बा हासिल करने की ग़र्ज़ से बंबई आया था। मेरी कंपनी की कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई। इधर एक्टरों के नाकामयाब होने से और भी नुकसान हुए। चुनांचे जयराज, बिब्बो, ताराबाई जैसे एक्टर भी किनारा-कश हो गए। सिनेमा से किसी सुधार की आशा करना बेकार है। यह कला भी उसी तरह पूँजीपतियों के हाथों में है, जैसे शराब फरोशी...। इनको इससे मतलब नहीं कि पब्लिक की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्हें तो अपनी पूँजी से मतलब है। नग्नता, नृत्य, चुंबन और मर्दों का औरतों पर हमला... ये सब इनकी नज़रों में जायज़ है। पब्लिक का स्तर भी इतना गिर गया है कि जब तक ये फार्मूले न हों, तो उनको फिल्म में मज़ा नहीं आता। फिल्मों में सुधार का बीड़ा कौन उठाए? मेरे विचार में सभ्य महिलाओं का फिल्मों में आना ठीक नहीं है, क्योंकि स्टूडियों की फ़िज़ा इनके लिए नहीं है और भविष्य में भी इसमें सुधार असंभव है।
हमारे सिनेमा वालों ने पुलिस वालों की मानसिकता से काम लेकर यह समझ लिया है कि भद्दे मसखरेपन में लड़ाई और जोर-आज़माइश या नकली ऊँची दीवार से कूदने में और झूठमूट में टीन की तलवार चलाने में ही जनता को आनंद आता है और कुछ उत्तेजना व चुंबन सिनेमा के लिए उतना ही जरूरी है, जितना जिस्म के लिए आँखें...। बेशक अवाम वीरता भरी जवांमर्दी देखना चाहती है; इश्क़, मुहब्बत भी उनके लिए आकर्षण रखता है, लेकिन यह ख्याल गलत है कि उत्तेजना व चुंबन के बगैर मुहब्बत का इज़हार हो नहीं सकता और सिर्फ तलवार चलाना ही जवांमर्दी है या बिना किसी जरूरत के गीत पेश करना जरूरी है। इन बातों से ही अवाम को खुशी मिलती है, तो यह इंसानियत की गलत कल्पना है।
- प्रेमचंद
....................................................................................................................................................................
( प्रेमचन्द जी हिन्दी सिनेमा के लिए कहानियाँ लिखने के उद्देश्य से जून 1934 ई. में बंबई गये थे। सिनेमा के गिरते स्तर को देखकर वे बहुत निराश हुए, इस पर उन्होंने एक लेख लिखा, जो उस समय प्रतिष्ठित पाकिस्तानी पत्रिका 'नक़्श' के जून, 1964 अंक में प्रकाशित हुआ था, इस दुर्लभ लेख को बाद में ‘दैनिक भास्कर’ समाचार पत्र ने 31 जुलाई 2005 को प्रकाशित किया था, यह दुर्लभ लेख है)
प्रस्तुति -डॉ. जगदीश व्योम